|
निधन
|
: |
4 अप्रैल 1987
तार सप्तक का प्रकाशन सन्
1943 में हुआ था। दूसरे संस्करण की भूमिका सन् 1963 में लिखी जा रही
है। बीस वर्ष की एक पीढ़ी मानी जाती है। वयमेव याता: के अनिवार्य
नियम के अधीन सप्तक के सहयोगी, जो 1943 के प्रयोगी थे, सन् 1963 के
सन्दर्भ हो गये हैं। दिक्कालजीवी को इसे नियति मान कर ग्रहण करना
चाहिए, पर प्रयोगशील कवि के बुनियादी पैंतरे में ही कुछ ऐसी बात थी
कि अपने को इस नये रूप में स्वीकार करना उसके लिए कठिन हो। बूढ़े सभी
होते हैं, लेकिन बुढ़ापा किस पर कैसा बैठता है यह इस पर निर्भर रहता
है कि उसका अपने जीवन से, अपने अतीत और वर्तमान से (और अपने भविष्य
से भी क्यों नहीं?) कैसा सम्बन्ध रहता है। हमारी धारणा है कि तार
सप्तक ने जिन विविध नयी प्रवृत्तियों को संकेतित किया था उनमें एक यह
भी रही कि कवि का युग-सम्बन्ध सदा के लिए बदल गया था। इस बात को ठीक
ऐसे ही सब कवियों ने सचेत रूप से अनुभव किया था, यह कहना झूठ होगा;
बल्कि अधिक सम्भव यही है कि एक स्पष्ट, सुचिन्तित विचार के रूप में
यह बात किसी भी कवि के सामने न आयी हो। लेकिन इतना असन्दिग्ध है कि
सभी कवि अपने को अपने समय से एक नये ढंग से बाँध रहे थे। उत्पत्स्यते
तु मम कोऽपि समानधर्मा वाला पैंतरा न किसी कवि के लिए सम्भव रहा था,
न किसी को स्वीकार्य था। सभी सबसे पहले समाजजीवी मानव प्राणी थे और
समानधर्मा का अर्थ उनके लिए कवि-धर्मा से पहले मानवधर्मा था। यह भेद
किया जा सकता है कि कुछ के लिए आधुनिकधर्मा होने का आग्रह पहले था और
अपनी मानवधर्मिता को वह आधुनिकता से अलग नहीं देख सकते थे, और दूसरे
कुछ ऐसे थे जिनके लिए आधुनिकता मानवधर्मिता का एक आनुषंगिक पहलू अथवा
परिणाम था।
सप्तक के कवियों का विकास अपनी-अपनी अलग दिशा में हुआ है। सर्जनशील
प्रतिभा का धर्म है कि वह व्यक्तित्व ओढ़ती है। सृष्टियाँ जितनी
भिन्न होती हैं स्रष्टा उससे कुछ कम विशिष्ट नहीं होते, बल्कि उनके
व्यक्तित्व की विशिष्टताएँ ही उनकी रचना में प्रतिबिम्बित होती हैं।
यह बात उन पर भी लागू होती है जिनकी रचना प्रबल वैचारिक आग्रह लिये
रहती है जब तक कि वह रचना है, निरा वैचारिक आग्रह नहीं है। कोरे
वैचारिक आग्रह में अवश्य ऐसी एकरूपता हो सकती है कि उसमें व्यक्तियों
को पहचानना कठिन हो जाये। जैसे शिल्पाश्रयी काव्य पर रीति हावी हो
सकती है, वैसे ही मताग्रह पर भी रीति हावी हो सकती है। सप्तक के
कवियों के साथ ऐसा नहीं हुआ, संपादक की दृष्टि में यह उनकी अलग-अलग
सफलता (या कि स्वस्थता) का प्रमाण है। स्वयं कवियों की राय इससे
भिन्न भी हो सकती है- वे जानें।
इन बीस वर्षों में सातों कवियों की परस्पर अवस्थिति में विशेष अन्तर
नहीं आया है। तब की सम्भावनाएँ अब की उपलब्धियों में परिणत हो गयी
हैं- सभी बोधिसत्त्व अब बुद्ध हो गये हैं। पर इन सात नये ध्यानी
बुद्धों के परस्पर सम्बन्धों में विशेष अन्तर नहीं आया है। अब भी
उनके बारे में उतनी ही सचाई के साथ कहा जा सकता है कि उनमें मतैक्य
नहीं है, सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग-अलग है-जीवन के
विषय में, समाज और धर्म, राजनीति के विषय में, काव्य-वस्तु और शैली
के, छन्द और तुक के, कवि के दायित्वों के-प्रत्येक विषय में उनका आपस
में मतभेद है। और यह बात भी उतनी ही सच है कि वे सब परस्पर एक-दूसरे
पर, दूसरे की रुचियों, कृतियों और आशाओं-विश्वासों पर और यहाँ तक कि
एक-दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हँसते हैं। (सिवा इसके कि इन
पंक्तियों को लिखते समय संपादक को जहाँ तक ज्ञान है कुत्ता किसी कवि
के पास नहीं है, और हँसी की पहले की सहजता में कभी कुछ व्यंग्य या
विद्रूप का भाव भी आ जाता होगा!)।
ऐसी परिस्थिति में ऐसा बहुत कम है जो निरपवाद रूप से सभी कवियों के
बारे में कहा जा सकता है। ये मनके इतने भिन्न हैं कि सबको किसी एक
सूत्र में गूँथने का प्रयास व्यर्थ ही होगा। कदाचित् एक
बात-मात्रा-भेद की गुंजाइश रख कर-सबके बारे में कही जा सकती है। सभी
चकित हैं कि तार सप्तक ने समकालीन काव्य-इतिहास में अपना स्थान बना
लिया है। प्राय: सभी ने यह स्वीकार भी कर लिया है। अपने कार्य का या
प्रगति का, मूल्यांकन जो भी जैसा भी कर रहा हो, जिसकी वर्तमान
प्रवृत्ति जो हो, सभी ने यह स्थिति लगभग स्वीकार कर ली है कि उन्हें
नगर के चौक में खम्भे से, या मील के पत्थर से, बाँध कर नमूना बनाया
जाये : यह देखो और इससे शिक्षा ग्रहण करो ! कम से कम एक कवि का मुखर
भाव ऐसा है, और कदाचित् दूसरों के मन में भी अव्यक्त रूप में हो, कि
अच्छा होता अगर मान लिया जा सकता कि वह तार सप्तक में संग्रहीत था ही
नहीं। इतिहास अपने चरित्रों या कठपुतलों को इसकी स्वतन्त्रता नहीं
देता कि वे स्वयं अपने को न हुआ मान लें। फिर भी मन का ऐसा भाव
लक्ष्य करने लायक और नहीं तो इसलिए भी है कि वह परवर्ती साहित्य पर
एक मन्तव्य भी तो है ही- समूचे साहित्य पर नहीं तो कम से कम सप्तक के
अन्य कवियों की कृतियों पर (और उससे प्रभावित दूसरे लेखन पर) तो
अवश्य ही। असम्भव नहीं कि संकलित कवियों को अब इस प्रकार एक-दूसरे से
सम्पृक्त होकर लोगों के सामने उपस्थित होना कुछ अजब या असमंजसकारी
लगता हो। लेकिन ऐसा है भी, तो उस असमंजस के बावजूद वे इस सम्पर्क को
सह लेने को तैयार हो गये हैं इसे संपादक अपना सौभाग्य मानता है। अपनी
ओर से वह यह भी कहना चाहता है कि स्वयं उसे इस सम्पृक्ति से कोई
संकोच नहीं है। परवर्ती कुछ प्रवृत्तियाँ उसे हीन अथवा आपत्तिजनक भी
जान पड़ती हैं, और नि:सन्देह इनमें से कुछ का सूत्र तार सप्तक से
जोड़ा जा सकता है या जोड़ दिया जाएगा; तथापि संपादक की धारणा है कि
तार सप्तक ने अपने प्रकाशन का औचित्य प्रमाणित कर लिया। उसका
पुनर्मुद्रण केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज को उपलभ्य बनाने के लिए नहीं,
बल्कि इसलिए भी संगत है कि परवर्ती काव्य-प्रगति को समझने के लिए
इसका पढऩा आवश्यक है। इन सात कवियों का एकत्रित होना अगर केवल संयोग
भी था तो भी वह ऐसा ऐतिहासिक संयोग हुआ जिसका प्रभाव परवर्ती
काव्य-विकास में दूर तक व्याप्त है।
इसी समकालीन अर्थवत्ता की पुष्टि के लिए प्रस्तुत संस्करण को केवल
पुनर्मुद्रण तक सीमित न रख कर नया संवद्र्धित रूप देने का प्रयत्न
किया गया है। तार सप्तक के ऐतिहासिक रूप की रक्षा करते हुए जहाँ पहले
की सब सामग्री-काव्य और वक्तव्य-अविकल रूप से दी जा रही है, वहाँ
प्रत्येक कवि से उसकी परवर्ती प्रवृत्तियों पर भी कुछ विचार प्राप्त
किए गये हैं। संपादक का विश्वास है कि यह प्रत्यवलोकन प्रत्येक कवि
के कृतित्व को समझने के लिए उपयोगी होगा और साथ ही तार सप्तक के पहले
प्रकाशन से अब तक के काव्य-विकास पर भी नया प्रकाश डालेगा। एक पीढ़ी
का अन्तराल पार करने के लिए प्रत्येक कवि की कम से कम एक-एक नयी रचना
भी दे दी गयी है। इसी नयी सामग्री को प्राप्त करने के प्रयत्न में
सप्तक इतने वर्षों तक अनुपलभ्य रहा : जिनके देर करने का डर था उनसे
सहयोग तुरन्त मिला; जिनकी अनुकूलता का भरोसा था उन्होंने ही सबसे देर
की-आलस्य या उदासीनता के कारण भी, असमंजस के कारण भी, और शायद
अनभिव्यक्त आक्रोश के कारण भी : जो पास रहे वे ही तो सबसे दूर रहे।
संपादक ने वह हठधर्मिता (बल्कि बेहयाई!) ओढ़ी होती जो पत्रकारिता (और
संपादन) धर्म का अंग है, तो सप्तक का पुनर्मुद्रण कभी न हो पाता : यह
जहाँ अपने परिश्रम का दावा है; वहाँ अपनी हीनतर स्थिति का स्वीकार भी
है।
पुस्तक के बहिरंग के बारे में अधिक कुछ कहना आवश्यक नहीं है। पहले
संस्करण में जो आदर्शवादिता झलकती थी, उसकी छाया कम से कम संपादक पर
अब भी है, किन्तु काव्य-प्रकाशन के व्यावहारिक पहलू पर नया विचार
करने के लिए अनुभव ने सभी को बाध्य किया है। पहले संस्करण से उपलब्धि
के नाम पर कवियों को केवल पुस्तक की कुछ प्रतियाँ ही मिलीं; बाकी जो
कुछ उपलब्धि हुई वह भौतिक नहीं थी! सम्भाव्य आय को इसी प्रकार के
दूसरे संकलन में लगाने का विचार भी उत्तम होते हुए भी वर्तमान
परिस्थिति में अनावश्यक हो गया है। रूप-सज्जा के बारे में भी स्वीकार
करना होगा कि नये संस्करण पर परवर्ती सप्तकों का प्रभाव पड़ा है। जो
अतीत की अनुरूपता के प्रति विद्रोह करते हैं, वे प्राय: पाते हैं कि
उन्होंने भावी की अनुरूपता पहले से स्वीकार कर ली थी! विद्रोह की ऐसी
विडम्बना कर सकना इतिहास के उन बुनियादी अधिकारों में से है जिसका वह
बड़े निर्ममत्व से उपयोग करता है। नये संस्करण से उपलब्धि कुछ तो
होगी, ऐसी आशा की जा सकती है। उसका उपयोग कौन कैसे करेगा यह योजनाधीन
न होकर कवियों के विकल्प पर छोड़ दिया गया। वे चाहें तो उसे तार
सप्तक का प्रभाव मिटाने में या उसके संसर्ग की छाप धो डालने में भी
लगा सकते हैं!
तार सप्तक का प्रकाशन जब
हुआ, तब मन में यह विचार ज़रूर उठा था कि इसी प्रकार की पुस्तकों का
एक अनुक्रम प्रकाशित किया जा सकता है, जिसमें क्रमश: नये आने वाले
प्रतिभाशाली कवियों की कविताएँ संगृहीत की जाती रहें-ऐसे कवियों की
जिनमें इतनी प्रतिभा तो है कि उनकी संगृहीत रचनाएँ प्रकाशित हों,
लेकिन जो इतने प्रतिष्ठापित नहीं हुए हैं कि कोई प्रकाशक सहसा उनके
अलग-अलग संग्रह निकाल दे। तार सप्तक का आयोजन भी मूलत: इसी भावना से
हुआ था, यद्यपि इसमें साथ ही यह आदर्शवादी आरोप भी था कि संग्रह का
प्रकाशन सहकार-मूलक हो। (जिन पाठकों ने संग्रह देखा है वे शायद स्मरण
करेंगे कि इस आदर्श की रक्षा तब भी नहीं हो सकी थी; दूसरा सप्तक में
तो उसे निबाहने का यत्न ही व्यर्थ मान लिया गया था।)
तो तार सप्तक के कवि ऐसे कवि थे, जिनके बारे में कम से कम संपादक की
यह धारणा थी कि उनमें कुछ है, और वे पाठक के सामने लाये जाने के
पात्र हैं; यद्यपि वे हैं नये ही, केवल कवियश:प्रार्थी ही और इसलिए
काव्यक्षेत्र के अन्वेषी ही। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनमें से सभी
अनन्तर काव्य-क्षेत्र में आगे बढ़े-कम से कम एक ने तो न केवल ऐलान कर
के कविता छोड़ दी बल्कि क्रमश: कविता के ऐसे आलोचक हो गये कि उसे
साहित्य-क्षेत्र से ही खदेड़ देने पर तुल गये; और बाकी में से दो-एक
और भी कविता से उपराम-से हैं! फिर भी, हम आज भी समझते हैं कि तार
सप्तक का प्रकाशन-प्रकाशन ही नहीं, उसका आयोजन, संकलन, संपादन-न केवल
समयोचित और उपयोगी था बल्कि उसे हिन्दी काव्य-जगत् की एक
महत्त्वपूर्ण घटना भी कहा जा सकता है। और आलोचकों द्वारा उसकी जितनी
चर्चा हुई है उसे सप्तक के प्रभाव का सूचक मान लेना कदाचित् अनुचित न
होगा।
दूसरा सप्तक में फिर सात नये कवियों की संगृहीत रचनाएँ प्रस्तुत की
जा रही हैं। सात में से कोई भी हिन्दी-जगत् का अपरिचित हो, ऐसा नहीं
है, लेकिन किसी का कोई स्वतन्त्र कविता-संग्रह नहीं छपा है, अत: यह
कहा जा सकता है कि प्रकाशित कविता-ग्रन्थों के जगत् में ये कवि इसी
पुस्तक के साथ प्रवेश कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि हिन्दी में
सम्प्रति जो काव्यसंग्रह छपते हैं; उनमें कम ऐसे होंगे जिनमें अच्छी
कविताओं की इतनी बड़ी संख्या एकत्र मिले जितनी दूसरा सप्तक में पायी
जाएगी।
क्या ये रचनाएँ प्रयोगवादी हैं? क्या ये कवि किसी एक दल के हैं, किसी
मतवाद-राजनीतिक या साहित्यिक-के पोषक हैं? प्रयोगवाद नाम के नये
मतवाद के प्रवर्तन का दायित्व क्यों कि अनचाहे और अकारण ही हमारे
मत्थे मढ़ दिया गया है, इसलिए हमारा इन प्रश्नों के उत्तर में कुछ
कहना आवश्यक है, और नहीं तो इसीलिए कि दूसरा सप्तक के संगृहीत कवि
आरम्भ से ही किसी पूर्वग्रह के शिकार न बनें, अपने कृतित्व के आधार
पर ही परखे जाएँ।
प्रयोग का कोई वाद नहीं है। हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं। न प्रयोग
अपने-आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं
है; कविता भी अपने-आप में इष्ट या साध्य नहीं है: अत: हमें
प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी
कहना। क्योंकि यह आग्रह तो हमारा है कि जिस प्रकार कविता-रूपी माध्यम
को बरतते हुए आत्माभिव्यक्ति चाहने वाले कवि को अधिकार है कि उस
माध्यम का अपनी आवश्यकता के अनुरूप श्रेष्ठ उपयोग करे, उसी प्रकार
आत्म-सत्य के अन्वेषी कवि को, अन्वेषण की विशेषताओं को परखने का भी
अधिकार है। इतना ही नहीं, बिना माध्यम की विशेषता, उसकी शक्ति और
उसकी सीमा को परखे और आत्मसात् किये उस माध्यम का श्रेष्ठ उपयोग हो
ही नहीं सकता। जो लोग प्रयोग की निन्दा करने के लिए परम्परा की दुहाई
देते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि परम्परा, कम से कम कवि के लिए, कोई
ऐसी पोटली बाँध कर अलग रखी हुई चीज़ नहीं है जिसे वह उठा कर सिर पर
लाद लेकर चल निकले। (कुछ आलोचकों के लिए भले ही वैसा हो।) परम्परा का
कवि के लिए कोई अर्थ नहीं है जब तक वह उसे ठोक-बजा कर, तोड़-मरोड़
कर, देख कर आत्मसात् नहीं कर लेता; जब तक वह एक इतना गहरा संस्कार
नहीं बन जाती कि उसका चेष्टापूर्वक ध्यान रख कर उसका निर्वाह करना
अनावश्यक न हो जाए। अगर कवि की आत्माभिव्यक्ति एक संस्कार-विशेष के
वेष्टन में ही सहज सामने आती है, तभी वह संस्कार देने वाली परम्परा
कवि की परमपरा है, नहीं तो-वह इतिहास है, शास्त्र है, ज्ञान-भंडार है
जिससे अपरिचित भी रहा जा सकता है। अपरिचित ही रहा जाए, ऐसा आग्रह
हमारा नहीं है-हम पर तो बौद्धिकता का आरोप लगाया जाता है!- पर उससे
अपरिचित रह कर भी परम्परा से अवगत हुआ जा सकता है और कविता की जा
सकती है।
तो प्रयोग अपने-आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। और दोहरा साधन है।
क्यों कि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित
करता है, दूसरे उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का
भी साधन है। अर्थात् प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह
जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प
दोनों के क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह इतनी सरल और सीधी
बात है कि इससे इनकार करना चाहना कोरा दुराग्रह है; ऐसे दुराग्रही
अनेक हैं और उस वर्ग में हैं जो साहित्य-शिक्षण का दायित्व लिये है,
इससे हमें आतंकित न होना चाहिए। जिस वर्ग की घोषित नीति यह है कि
उसके द्वारा ग्राह्य होने के लिए कोई वस्तु या रचना तीन सौ वर्ष
पुरानी तो होनी ही चाहिए, उस वर्ग से आज की कविता पर बहस कर के क्या
लाभ? उससे तो तीन सौ वर्ष बाद बात करना अलम् होगा-और तब कदाचित् वह
अनावश्यक होगा क्यों कि आज का प्रयोग तब की परम्परा हो गयी होगी-उनकी
परम्परा! छायावाद जब एक जीवित अभिव्यक्ति था, तब वह जिन्हें अग्राह्य
था, आज वे उसके समर्थक और प्रतिपादक हं जब वह मृत हो चुका; आज वे उसे
उनसे बचाना चाहते हैं जिनमें आज का जीवित सत्य अभिव्यक्ति खोज रहा
है, भले ही अटपटे शब्दों में।
प्रयोग का हमारा कोई वाद नहीं है, इसको और भी स्पष्ट करने के लिए एक
बात हम और कहें। प्रयोग निरन्तर होते आये हैं, और प्रयोगों के द्वारा
ही कविता या कोई भी कला, कोई भी रचनात्मक कार्य, आगे बढ़ सका है। जो
कहता है कि मैंने जीवन-भर कोई प्रयोग नहीं किया, वह वास्तव में यही
कहता है कि मैंने जीवनभर कोई रचनात्मक कार्य करना नहीं चाहा; ऐसा
व्यक्ति अगर सच कहता है तो यही पाया जाएगा कि उसकी कविता कविता नहीं
है, उसमें रचनात्मकता नहीं है; वह कला नहीं, शिल्प है, हस्तलाघव है।
जो उसी को कविता मानना चाहते हैं, उससे हमारा झगड़ा नहीं है। झगड़ा
हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारी भाषाएँ भिन्न हैं, और झगड़े के लिए
भी साधारणीकरण अनिवार्य है! लेकिन इस आग्रह पर स्थिर रहते हुए भी
हमें यह भी कहना चाहिए कि केवल प्रयोगशीलता ही किसी रचना को काव्य
नहीं बना देती। हमारे प्रयोग का पाठक या सहृदय के लिए कोई महत्त्व
नहीं है, महत्त्व उस सत्य का है जो प्रयोग द्वारा हमें प्राप्त हो।
हमने सैकड़ों प्रयोग किए हैं यह दावा लेकर हम पाठक के सामने नहीं जा
सकते, जब तक हम यह न कह सकते हों कि देखिए, हमने प्रयोग द्वारा यह
पाया है। प्रयोगों का महत्त्व कत्र्ता के लिए चाहे जितना हो, सत्य की
खोज, लगन, उसमें चाहे जितनी उत्कट हो, सहृदय के निकट वह सब
अप्रासंगिक है। पारखी मोती परखता है, गोताखोर के असफल उद्योग नहीं।
गोताखोर का परिश्रम या प्रयोग अगर प्रासंगिक हो सकता है तो मोती को
सामने रख कर ही-इस मोती को पाने में इतना परिश्रम लगा-बिना मोती पाये
उसका कोई महत्त्व नहीं है।
इस प्रकार प्रयोग का वादा और भी बेमानी हो जाता है। जो सत्य को शोध
में प्रयोग करता है वह खूब जानता है कि उसके प्रयोग उसके निकट
जीवन-मरण का ही प्रश्न क्यों न हों, दूसरों के लिए उनका कोई महत्त्व
नहीं। महत्त्व होगा शोध के परिणाम का। और वह यह भी जानता है कि ऐसा
ही ठीक है। स्वयं वह भी उस सत्य को अधिक महत्त्व देता है, नहीं तो उस
शोध में इतना संलग्न न होता।
हम समझते हैं कि इस भूमिका के बाद उन आक्षेपों का उत्तर देना
अनावश्यक हो जाता है जो हमें प्रयोगवाद कह कर हम पर किये गये हैं।
कुछ आक्षेपों को पढ़ कर तो बड़ा क्लेश होता है, इसलिए नहीं कि उनमें
कुछ तत्त्व है, इसलिए कि उनमें तर्क-परिपाटी की ऐसी अद्भुत विकृति
दीखती है, जो आलोचक से अपेक्षित नहीं होती। आलोचक में पूर्वग्रह हो
सकता है; पर कम से कम तर्क-पद्धति का ज्ञान उसे होगा, और उसे वह
विकृत नहीं करेगा, ऐसी आशा उससे अवश्य की जाती है। श्री नन्ददुलारे
वाजपेयी का प्रयोगवादी रचनाएँ शीर्षक निबन्ध तर्क-विकृति का
आश्चर्यजनक उदाहरण है। इस प्रकार के आक्षेपों का उत्तर देना एक
निष्फल प्रयोग होगा; और हम कह चुके कि निष्फल प्रयोगों का कोई
सार्वजनिक महत्त्व नहीं है। लेकिन साधारणीकरण के प्रश्न पर कुछ विचार
कर लेना कदाचित् उचित होगा।
तार सप्तक के कवियों पर यह आक्षेप किया गया कि वे साधारणीकरण का
सिद्धान्त नहीं मानते। यह दोहरा अन्याय है। क्यों कि वे न केवल इस
सिद्धान्त को मानते हैं बल्कि इसी से प्रयोगों की आवश्यकता भी सिद्ध
करते हैं। यह मानना होगा कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ हमारी
अनुभूतियों का क्षेत्र भी विकसित होता गया है और अनुभूतियों को
व्यक्त करने के हमारे उपकरण भी विकसित होते गये हैं। यह कहा जा सकता
है कि हमारे मूल राग-विराग नहीं बदले-प्रेम अब भी प्रेम है और घृणा
अब भी घृणा, यह साधारणतया स्वीकार किया जा सकता है। पर यह भी ध्यान
में रखना होगा कि राग वही रहने पर भी रागात्म्क सम्बन्धों की
प्रणालियाँ बदल गयी हैं; और कवि का क्षेत्र रागात्मक सम्बन्धों का
क्षेत्र होने के कारण इस परिवर्तन का कवि-कर्म पर बहुत गहरा असर पड़ा
है। निरे तथ्य और सत्य में-या कह लीजिए वस्तु-सत्य और व्यक्ति-सत्य
में-यह भेद है कि सत्य वह तथ्य है जिसके साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध
है; बिना इस सम्बन्ध के वह एक बाह्य वास्तविकता है जो तद्वत् काव्य
में स्थान नहीं पा सकती। लेकिन जैसे-जैसे बाह्य वास्तविकता बदलती
है-वैसे-वैसे हमारे उससे रागात्मक सम्बन्ध जोडऩे की प्रणालियाँ भी
बदलती हैं और अगर नहीं बदलतीं तो उस बाह्य वास्तविकता से हमारा
सम्बन्ध टूट जाता है। कहना होगा कि जो आलोचक इस परिवर्तन को नहीं समझ
पा रहे हैं, वे उस वास्तविकता से टूट गये हैं जो आज की वास्तविकता
है। उससे रागात्मक सम्बन्ध जोडऩे में असमर्थ वे उसे केवल बाह्य
वास्तविकता मानते हैं जबकि हम उससे वैसा सम्बन्ध स्थापित करके उसे
आन्तरिक समय बना लेते हैं। और इस विपर्यय से साधारणीकरण की नयी
समस्याएँ आरम्भ होती हैं। प्राचीन काल में, जब ज्ञान का क्षेत्र
सीमित था और अधिक संहत था, जब कवि, वैज्ञानिक, साहित्यिक आदि अलग-अलग
बिल्ले अनावश्यक थे और जो पठित या शिक्षित था, सभी ज्ञानों का पारंगत
नहीं तो परिचित था ही, साधारणीकरण की समस्या दूसरे प्रकार की थी। तब
भाषा का केवल एक मुहावरा था। या कह लीजिए कि शिक्षित वर्ग का एक
मुहावरा था, जन का एक और। एक संस्कृत था, एक प्राकृत। लेकिन आज क्या
वह स्थिति है? विशेष ज्ञानों के इस युग में भाषा एक रहते हए भी उसके
मुहावरे अनेक हो गये हैं। भाषा आज भी प्रेषण का माध्यम है; यह कोई
नहीं कहता कि उसने अपनी सार्वजनिकता की प्रवृत्ति छोड़ दी है या छोड़
दे। लेकिन वह अब प्रवृत्ति है, तथ्य नहीं। ऐसी कोई भाषा नहीं है जो
सब समझते हों, सब बोलते हों। अँग्रेज़ी है, अँग्रेज़ी के बड़े-बड़े
कोश हैं जो शब्दों के सर्व-सम्मत अर्थ देते हैं, पर गणितज्ञ की
अँग्रेज़ी दूसरी है, अर्थशास्त्री की दूसरी और उपन्यासकार की दूसरी।
ऐसी स्थिति में जो कवि एक क्षेत्र का सीमित सत्य (तथ्य नहीं, सत्य :
अर्थात् उस सीमित क्षेत्र में जिस तथ्य से रागात्मक सम्बध है वह) उसी
क्षेत्र में नहीं, उस से बाहर अभिव्यक्त करना चाहता है, उसके सामने
बड़ी समस्या है। या तो वह यह प्रयत्न ही छोड़ दे; सीमित सत्य को
सीमित क्षेत्र में सीमित मुहावरे के माध्यम से अभिव्यक्त करे-यानी
साधारणीकरण तो करे पर साधारण का क्षेत्र संकुचित कर दे-अर्थात् एक
अन्तर्विरोध का आश्रय ले; या फिर वह बृहत्तर क्षेत्र तक पहुँचने का
आग्रह न छोड़े और इसलिए क्षेत्र के मुहावरे से बँधा न रह कर उससे
बाहर जाकर राह खोजने की जोख़िम उठाए। इस प्रकार वह साधारणीकरण के लिए
ही एक संकुचित क्षेत्र का साधारण मुहावरा छोडऩे को बाध्य
होगा-अर्थात् एक दूसरे अन्तर्विरोध की शरण लेगा? यदि यह निरूपण ठीक
है, तो प्रश्न इतना ही है कि दोनों अन्तर्विरोधों में से कौन-सा अधिक
ग्राह्य-या कम अग्राह्य-है। हम इतना ही कहेंगे कि जो दूसरा पथ चुनता
है उसे कम से कम एक अधिक उदार, अधिक व्यापक दृष्टि से देखने या देखना
चाहने का श्रेय तो मिलना चाहिए-उसके साहस को आप साहसिकता कह लीजिए पर
उसकी नीयत को बुरा आप कैसे कह सकते हैं?
ज़रा भाषा के मूल प्रश्न पर-शब्द और उसके अर्थ के सम्बन्ध पर-ध्यान
दीजिए। शब्द में अर्थ कहाँ से आता है, क्यों और कैसे बदलता है, अधिक
या कम व्याप्ति पाता है? शब्दार्थ-विज्ञान का विवेचन यहाँ अनावश्यक
है; एक अत्यन्त छोटा उदाहरण लिया जाए। हम कहते हैं, गुलाबी, और उससे
एक विशेष रंग का बोध हमें होता है। निस्सन्देह इसका अभिप्राय है
गुलाब के फूल के रंग जैसा रंग; यह उपमा उसमें निहित है। आरम्भ में
गुलाबी शब्द से उसे उस रंग तक पहुँचने के लिए गुलाब के फूल की
मध्यस्थता अनिवार्य रही होगी; उपमा के माध्यम से ही अर्थ लाभ होता
रहा होगा। उस समय यह प्रयोग चामत्कारिक रहा होगा। पर अब वैसा नहीं
है। अब हम शब्द से सीधे रंग तक पहुँच जाते हैं; फूल की मध्यस्थता
अनावश्यक है। अब उस अर्थ का चमत्कार मर गया है, अब वह अभिधेय हो गया
है। और अब इससे भी अर्थ में कोई बाधा नहीं होती कि हम जानते हैं,
गुलाब कई रंगों का होता है-सफेद, पीला, लाल, यहाँ तक कि लगभग काला
तक। यह क्रिया भाषा में निरन्तर होती रहती है और भाषा के विकास की एक
अनिवार्य क्रिया है। चमत्कार मरता रहता है और चामत्कारिक अर्थ अभिधेय
बनता रहता है। यों कहें कि कविता की भाषा निरन्तर गद्य की भाषा होती
जाती है। इस प्रकार कवि के सामने हमेशा चमत्कार की सृष्टि की समस्या
बनी रहती है-वह शब्दों को निरन्तर नया संस्कार देता चलता है और वे
संस्कार क्रमश: सार्वजनिक मानस में पैठ कर फिर ऐसे हो जाते हैं कि-उस
रूप में-कवि के काम के नहीं रहते। बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट
जाता है। कालिदास ने जब रघुवंश के आरम्भ में कहा था :
वागर्थाविवसम्पृक्तौ
वागर्थप्रतिपत्तये
जगत: पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ
तब इस बात को उन्होंने समझा
था और इसीलिए वाक् में अर्थ की प्रतिपत्ति की प्रार्थना की थी। जो
अभिधेय है, जो अर्थ वाक् में है ही, उसकी प्रतिपत्ति की प्रार्थना
कवि नहीं करता! अभिधेयार्थयुक्त शब्द तो वह मिट्टी, वह कच्चा माल है
जिससे वह रचना करता है; ऐसी रचना जिसके द्वारा वह अपना नया अर्थ
उसमें भर सके, उसमें जीवन डाल सके। यही वह अर्थ-प्रतिपत्ति है जिसके
लिए कवि वागर्थाविवसम्पृक्त पार्वती-परमेश्वर की वन्दना करता है। और
इस प्रार्थना को निरा वैचित्र्य या नयेपन की खोज कह कर उड़ाना चाहना
कवि-कर्म को बिलकुल न समझते हुए उसकी अवहेलना करना है। जब चामत्कारिक
अर्थ मर जाता है और अभिधेय बन जाता है तब उस शब्द की रागोत्तेजक
शक्ति भी क्षीण हो जाती है। उस अर्थ से रागात्मक सम्बन्ध नहीं
स्थापित होता। कवि तब उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुन: राग
का संचार हो, पुन: रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हो। साधारणीकरण का अर्थ
यही है। नहीं तो, अगर भाव भी वही जाने पुराने हैं, रस भी, और
संचारी-व्यभिचारी सबकी तालिकाएँ बन चुकी हैं तो कवि के लिए नया करने
को क्या रह गया है? क्या है जो कविता को आवृत्ति नहीं, सृष्टि का
गौरव दे सकता है? कवि नये तथ्यों को उनके साथ नये रागात्मक सम्बन्ध
जोड़ कर नये सत्यों का रूप दे, उन नये सत्यों को प्रेष्य बना कर उनका
साधारणीकरण करे, यही नयी रचना है। इसे नयी कविता का कवि नहीं भूलता।
साधारणीकरण का आग्रह भी उसका कम नहीं है; बल्कि यह देख कर कि आज
साधारणीकरण अधिक कठिन है यह अपने कर्तव्य के प्रति अधिक सजग है और उस
की पूर्ति के लिए अधिक बड़ा जोखिम उठाने को तैयार है। यह किसी हद तक
ठीक है कि जहाँ कवि की संवेदनाएँ अधिक उलझी हुई हैं वहाँ ग्राहक या
सहृदय में भी उन्हीं परिस्थितियों के कारण वैसा ही परिवर्तन हुआ है
और इसलिए कवि को प्रेषण की कुछ सुविधा भी मिलती है। पर ऊपर ज्ञान के
विशेष विभाजनों की जो बात कही गयी है उसका हल इसमें नहीं है, बल्कि
यह प्रश्न और भी जटिल हो जाता है। आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की समूची
प्रगति और प्रवृत्ति विशेषीकरण की है, इस बात को पूरी तरह समझ कर ही
यह अनुभव किया जा सकता है कि साधारणीकरण का काम कितना कठिनतर हो गया
है-समूचे ज्ञान-विज्ञान की विशेषीकरण की प्रवृत्ति को उलाँघ कर, उससे
ऊपर उठ कर, कवि को विभाजित सत्य को समूचा देखना और दिखाना है। इस
दायित्व को वह नहीं भूलता है। लेकिन यह बात उस की समझ में नहीं आती
कि वह तब तक के लिए कविता को छोड़ दे जब तक कि सारा ज्ञान फिर एक
होकर सब की पहुँच में न आ जाये-सब अलग-अलग मुहावरे फिर एक होकर एक
भाषा, एक मुहावरा के नारे के अधीन न हो जाएँ। उसे अभी कुछ कहना है
जिसे वह महत्त्वपूर्ण मानता है, इसलिए वह उसे उनके लिए कहता है जो
उसे समझें, जिन्हें वह समझा सके; साधारणीकरण को उसने छोड़ नहीं दिया
है पर वह जितनों तक पहुँच सके उन तक पहुँचता रह कर और आगे जाना चाहता
है, उनको छोड़ कर नहीं। असल में देखें तो वही परम्परा को साथ लेकर
चलना चाहता है, क्यों कि वह कभी उसे युग सेकट कर अलग होने नहीं देता,
जब कि उसके विरोधी परिणामत: यह कहते हैं कि कल का सत्य कल सब समझते
थे, आज का सत्य अगर आज सब एक साथ नहीं समझते तो हम उसे छोड़ कर कल ही
का सत्य कहें- बिना यह विचारे कि कल के उस सत्य की आज क्या
प्रासंगिकता है, आज कौन उसके साथ तुष्टिकर रागात्मक सम्बन्ध जोड़
सकता है!
(2)
यहाँ तक हम तार सप्तक और
उसकी उत्तेजनाप्रसूत आलोचनाओं से उलझते रहे हैं। दूसरा सप्तक की
भूमिका को इससे आगे जाना चाहिए। बल्कि यहाँ से उसे आरम्भ करना चाहिए,
क्यों कि एक पुस्तक की सफाई दूसरी पुस्तक की भूमिका में देना दोनों
के साथ थोड़ा अन्याय करना है। हम यहाँ तार सप्तक का उल्लेख कर के
आलोचकों के तत्सम्बन्धी पूर्वग्रहों को इधर न आकृष्ट करते, यदि यह
अनुभव न करते कि दोनों पुस्तकों का नाम-साम्य और दोनों का एक
संपादकत्व ही इसके लिए काफ़ी होगा। उन पूर्वग्रहों का आरोप अगर होना
ही है, तो क्यों न उनका उत्तर देते चला जाय?
दूसरा सप्तक के कवियों में संपादक स्वयं एक नहीं है, इससे उसका कार्य
कुछ कम कठिन हो गया है। कवियों के बारे में कुछ कहने में एक ओर हमें
संकोच कम होगा, दूसरी ओर आप भी हमारी बात को आसानी से एक ओर रख कर
कविताओं पर स्वयं अपनी राय कायम कर सकेंगे। इन नये कवियों को भी
कदाचित् प्रयोगवादी कह कर उनकी अवहेलना की जाए, या-जैसा कि पहले भी
हुआ- अवहेलना के लिए यही पर्याप्त समझा जाए कि इन कवियों ने जो
प्रयोग किये हैं वे वास्तव में नये नहीं हैं, प्रयोग नहीं हैं। ऐसा
कहना इन कवियों के बारे में उतना ही उचित या अनुचित होगा जितना कि
पहले सप्तक के; हमारी धारणा है कि उससे भी कम उचित होगा। यद्यपि सब
कवियों में भाषा का परिमार्जन और अभिव्यक्ति की सफाई एक-सी नहीं है
और अटपटेपन की झाँकी न्यूनाधिक मात्रा में प्रत्येक में मिलेगी,
तथापि सभी को ऐसी उपलब्धि हुई है जो प्रयोग को सार्थक करती है।
प्रयोग के लिए प्रयोग इनमें से भी किसी ने नहीं किया है पर नयी
समस्याओं और नये दायित्वों का तकाजा सबने अनुभव किया है और उससे
प्रेरणा सभी को मिला है। दूसरा सप्तक नये हिन्दी काव्य को निश्चित
रूप से एक कदम आगे ले जाता है और कृतित्व की दृष्टि से लगभग सूने आज
के हिन्दी क्षेत्र में आशा की नयी लौ जगाता है। ये कवि भी विरामस्थल
पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उनके आगे प्रशस्त पथ है और एक आलोकित
क्षितिज-रेखा। गुप्त, प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी, बच्चन, दिनकर;
इस सूची को हम आगे बढ़ावेंगे तो निस्सन्देह दूसरा सप्तक के कुछ
कवियों का उल्लेख उसमें होगा। और, फुटकर कविताओं को लें तो, जैसा कि
हम ऊपर भी कह आवे हैं, एक जिल्द में संख्या में इतनी अच्छी कविताएँ
इधर के प्रकाशनों में कम नजर आएँगी।
यह फिर कहना आवश्यक है कि इन
सात कवियों का एकत्र होना किसी दल या गुट के संगठन का सूचक नहीं है।
पहली बार हमने कवियों के आपसी मतभेद की बात की थी; नन्ददुलारे जी ने
यह परिणाम निकाला कि प्रयोगवादी कविता उन कवियों की कविता होती है
जिन में आपस में मतभेद हो; अब हम कहें कि प्रस्तुत संग्रह में ऐसे भी
कवि हैं जिन्हें हमने आज तक देखा ही नहीं, तो कदाचित् उन्हें
प्रयोगवाद की एक नयी परिभाषा यह भी मिल जाए कि प्रयोगवादी वे होते
हैं जो एक-दूसरे का मुँह देखे बिना एक-सी कविता लिखते हैं! उन्हें यह
अवसर देने में हमें संकोच नहीं, उन के तर्क पढऩे में रोचक हैं और
उत्तर की अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन कहना हम यह चाहते हैं कि ये सात
कवि भी विचार-साम्य या समान राजनीतिक या साहित्यिक मतवाद के कारण
एकत्र नहीं हुए या किये गये। कुछ से हमारा व्यक्तिगत परिचय भी हुआ
अवश्य, पर उनके यहाँ एकत्र होने का कारण उनकी कविता ही है। उसी की
शक्ति ने हमें आकृष्ट किया और उसी का सौन्दर्य इस सप्तक की मूल
प्रेरणा है। कवियों की ओर से इस संग्रह में भी उतना ही कम, उतना ही
अन्यमनस्क और विलम्बित सहयोग मिला जितना पहले सप्तक में मिला था;
बल्कि इस बार कठिनाई कुछ अधिक थी क्योंकि इस बार प्रस्ताव उनका नहीं
था कि एक सहकारी प्रकाशन किया जाय, इस बार हमारा आग्रह था कि नये
काव्य का एक प्रतिनिधि संग्रह निकाला जाय। जो हो, संग्रह आप के सामने
है; आप कविताओं को उन्हीं के गुण-दोष के आधार पर देखें; उन्हीं से
कवि की सफलता-असफलता और उसके आदर्शों की परख करें! हमने जो कुछ कहा,
इसी आशा से कि आप आलोचकों द्वारा आरोपित पूर्वग्रहों की मैली ओट से
इन्हें न देखें, अपनी स्वच्छ सहृदयता से ही देखें; हमारा विश्वास है
कि इस संग्रह से आपको तृप्ति मिलेगी।
तार सप्तक की भूमिका
प्रस्तुत करते समय इन पंक्तियों के लेखक में जो उत्साह था, उसमें
संवेदना की तीव्रता के साथ निस्सन्देह अनुभवहीनता का साहस भी रहा
होगा। संवेदना की तीव्रता अब कम हो गयी है, ऐसा हम नहीं मानना चाहते;
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अनुभव ने नये कवियों का संकलन प्रस्तुत
करते समय दुविधा में पडऩा सिखा दिया है। यह नहीं कि तीसरा सप्तक के
कवियों की संगृहीत रचनाओं के बारे में हम उससे कम आश्वस्त, या उनकी
सम्भावनाओं के बारे में कम आशामय हैं जितना उस समय तार सप्तक के
कवियों के बारे में थे। बल्कि एक सीमा तक इससे उलटा ही सच होगा। हम
समझते हैं कि तीसरा सप्तक के कवि अपने-अपने विकास-क्रम में अधिक
परिपक्व और मँजे हुए रूप में ही पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं। भविष्य
में इनमें से कौन कितना और आगे बढ़ेगा, यह या तो ज्योतिषियों का
क्षेत्र है या स्वयं उनके अध्यवसाय का। तीसरा सप्तक के कवि भी एक ही
मंज़िल तक पहुँचे हों, या एक ही दिशा में चले हों, या अपनी अलग दिशा
में भी एक-सी गति से चले हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। नि:सन्देह तार
सप्तक में भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि संगृहीत कवि सब अपनी-अपनी
अलग राह का अन्वेषण कर रहे हैं।
दुविधा और संकोच का कारण
दूसरा है। तार सप्तक के कवि अपनी रचना के ही प्रारम्भिक युग में
नहीं, एक नयी प्रवृत्ति की प्रारम्भिक अवस्था में सामने आये थे। पाठक
के सम्मुख उनके कृतित्व की माप-जोख करने के लिए कोई बने-बनाये मापदंड
नहीं थे। उनकी तुलना भी पूर्ववर्ती या समवर्ती दिग्गजों से नहीं की
जा सकती थी-क्यों कि तुलना के कोई आधार ही अभी नहीं बने थे। इसलिए
जहाँ उनकी स्थिति झारखंड की झाड़ी पर अप्रत्याशित फले हुए वन-कुसुम
की-सी अकेली थी, वहाँ उन्हें यह भी सुविधा थी कि उन के यत्किंचित्
अवदान की माप झारखंड के ही सन्दर्भ में हो सकती थी-दूर के उद्यानों
से कोई प्रयोजन नहीं था।
अब वह परिस्थिति नहीं है।
द्विवेदी काल के श्री मैथिलीशरण गुप्त या छायावादी युग के श्री
निराला जैसा कोई शलाका-पुरुष नयी कविता ने नहीं दिया है (न उसे अभी
इतना समय ही मिला है); फिर भी तुलना के लिए और नहीं तो पहले दोनों
सप्तकों के कवि हैं ही, और परम्पराओं की कुछ लीकें भी बन गयी हैं।
पत्र-पत्रिकाओं में नयी कविता ग्राह्य हो गयी है, संपादक-गण (चाहे
आतंकित होकर ही!) उसे अधिकाधिक छापने लगे हैं, और उसकी अपनी अनेक
पत्रिकाएँ और संकलन-पुस्तिकाएँ निकलने लगी हैं। उधर उसकी आलोचना भी
छपने लगी है, और धुरन्धर आलोचकों ने भी उसके अस्तित्व की चर्चा करना
गवारा किया है-चाहे अधिकतर भर्त्सना का निमित्त बना कर ही।
और कृतिकारों का अनुधावन करने वाली, स्वल्प पूँजी वाली प्रतिभाएँ भी
अनेक हो गयी हैं।
कहना न होगा कि इन सब कारणों से नयी कविता का अपने पाठक के और स्वयं
अपने प्रति उत्तरदायित्व बढ़ गया है। यह मान कर भी कि शास्त्रीय
आलोचकों से उसे सहानुभूतिपूर्ण तो क्या, पूर्वग्रहरहित अध्ययन भी
नहीं मिला है, यह आवश्यक हो गया है कि स्वयं उसके आलोचक तटस्थ और
निर्मम भाव से उसका परीक्षण करें। दूसरे शब्दों में परिस्थिति की
माँग यह है कि कविगण स्वयं एक-दूसरे के आलोचक बन कर सामने आवें।
पूर्वग्रह से मुक्त होना हर
समय कठिन है। फिर अपने ही समय की उस प्रवृत्ति के विषय में, जिससे
आलोचक स्वयं सम्बद्ध है, तटस्थ होना और भी कठिन है। फिर जब समीक्षक
एक ओर यह भी अनुभव करे कि वह प्रवृत्ति विरोधी वातावरण से घिरी हुई
है और सहानुभूति ही नहीं, समर्थन और वकालत भी माँगती है, तब उसकी
कठिनाई की कल्पना की जा सकती है।
लेकिन फिर भी नयी कविता अगर
इस काल की प्रतिनिधि और उत्तरदायी रचना-प्रवृत्ति है, और समकालीन
वास्तविकता को ठीक-ठीक प्रतिबिम्बित करना चाहती है, तो उसे स्वयं आगे
बढक़र यह त्रिगुण दायित्व ओढ़ लेना होगा। कृतिकार के रूप में नये कवि
को साथ-साथ वकील और जज दोनों होना होगा। (और संपादक होने पर साथ-साथ
अभियोक्ता भी!)
तीसरा सप्तक के संपादन की
कठिनाई के मूल में यही परिस्थिति है। तार सप्तक एक नयी प्रवृत्ति का
पैरवीकार माँगता था, इससे अधिक विशेष कुछ नहीं। तीसरा सप्तक तक
पहुँचते न पहुँचते प्रवृत्ति की पैरवी अनावश्यक हो गयी है, और कवियों
की पैरवी का तो सवाल ही क्या है? इस बात का अधिक महत्त्व हो गया है
कि संकलित रचनाओं का मूल्यांकन संपादक स्वयं न भी करे तो कम-से-कम
पाठक की इसमें सहायता अवश्य करे।
नयी कविता की प्रयोगशीलता का पहला आयाम भाषा से सम्बन्ध रखता है।
निस्सन्देह जिसे अब नयी कविता की संज्ञा दी जाती है वह भाषा-सम्बन्धी
प्रयोगशीलता को वाद की सीमा तक नहीं ले गयी है-बल्कि ऐसा करने को
अनुचित भी मानती रही है। यह मार्ग प्रपद्यवादी ने अपनाया जिसने घोषणा
की कि चीज़ों का एकमात्र नाम होता है और वह (प्रपद्यवादी कवि)
प्रयुक्त प्रत्येक शब्द और छन्द का स्वयं निर्माता है।
नयी कविता के कवि को इतना मानने में कोई कठिनाई न होती कि कोई शब्द
किसी दूसरे शब्द का सम्पूर्ण पर्याय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक
शब्द के अपने वाच्यार्थ के अलावा अलग-अलग लक्षणाएँ और व्यंजनाएँ होती
हैं-अलग संस्कार और ध्वनियाँ। किन्तु प्रत्येक वस्तु का अपना एक नाम
होता है, इस कथन को उस सीमा तक ले जाया जा सकता है जहाँ कि भाषा का
एक नया रहस्यवाद जन्म ले ले और अल्लाह के निन्यानबे नामों से परे
उसके अनिर्वचनीय सौवें नाम की तरह हम प्रत्येक वस्तु के सौवें नाम की
खोज में डूब जाएँ। भाषा-सम्बन्धी यह निन्यानबे का फेर प्रेषणीयता का
और इसलिए भाषा का ही बहुत बड़ा शत्रु हो सकता है। शब्द अपने-आप में
सम्पूर्ण या आत्यन्तिक नहीं है; किसी शब्द का कोई स्वयम्भूत अर्थ
नहीं है। अर्थ उसे दिया गया है, वह संकेत है जिसमें अर्थ की
प्रतिपत्ति की गयी है। एकमात्र उपयुक्तशब्द की खोज करते समय हमें
शब्दों की यह तदर्थता नहीं भूलनी होगी : वह एकमात्र इसी अर्थ में है
कि हमने (प्रेषण को स्पष्ट, सम्यक और निर्भ्रम बनाने के लिए) नियत कर
दिया है कि शब्द-रूपी अमुक एक संकेत का एकमात्र अभिप्रेत क्या होगा।
यहाँ यह मान लें कि शब्द के प्रति यह नयी, और कह लीजिए मानववादी
दृष्टि है; क्यों कि जो व्यक्ति शब्द का व्यवहार कर के शब्द में यह
प्रार्थना कर सकता था कि अनजाने उसमें बसे देवता के प्रति कोई अपराध
हो गया हो तो देवता क्षमा करे वह इस निरूपण को स्वीकार नहीं कर
सकता-नहीं मान सकता कि शब्द में बसने वाला देवता कोई दूसरा नहीं है,
स्वयं मानव ही है जिसने उसका अर्थ निश्चित किया है। यह ठीक है कि
शब्द को जो संस्कार इतिहास की गति में मिल गये हैं उन्हें मानव के
दिये हुए कहना इस अर्थ में सही नहीं है कि उनमें मानव का संकल्प नहीं
था-फिर भी वे मानव द्वारा व्यवहार के प्रसंग में ही शब्द को मिले हैं
और मानव से अलग अस्तित्व नहीं रख पा सकते थे।
किन्तु एकमात्र सही नाम वाली स्थापना को इस तरह मर्यादित करने का यह
अर्थ नहीं है कि किसी शब्द का सर्वत्र, सर्वदा सभी के द्वारा ठीक एक
ही रूप में व्यवहार होता है-बल्कि यह तो तभी होता जब कि वास्तव में
एक चीज़ का एक ही नाम होता और एक नाम की एक ही चीज़ होती! प्रत्येक
शब्द का प्रत्यक समर्थ उपयोक्ता उसे नया संस्कार देता है। इसी के
द्वारा पुराना शब्द नया होता है-यही उसका कल्प है। इसी प्रकार शब्द
वैयक्तिक प्रयोग भी होता है और प्रेषण का माध्यम भी बना रहता है,
दुरूह भी होता है और बोधगम्य भी, पुराना परिचित भी रहता है और
स्फूर्तिप्रद अप्रत्याशित भी।
नये कवि की उपलब्धि और देन की कसौटी इसी आधार पर होनी चाहिए।
जिन्होंने शब्द को नया कुछ नहीं दिया है, वे लीक पीटने वाले से अधिक
कुछ नहीं हैं-भले ही जो लीक वह पीट रहे हैं वह अधिक पुरानी न हो। और
जिन्होंने उसे नया कुछ देने के आग्रह में पुराना बिलकुल मिटा दिया
है, वे ऐसे देवता हैं जो भक्तको नया रूप दिखाने के लिए अन्तर्धान ही
हो गये हैं! कृतित्व का क्षेत्र इन दोनों सीमा-रेखाओं के बीच में है।
यह ठीक है कि बीच का क्षेत्र बहुत बड़ा है, और उसमें कोई इस छोर के
निकट हो सकता है तो कोई उस छोर के। दुरूहता अपने-आप में कोई दोष नहीं
है, न अपने-आप में इष्ट है। इस विषय को लेकर झगड़ा करना वैसा ही है
जैसा इस चर्चा में कि सुराही का मुँह छोटा है या बड़ा, यह न देखना कि
उसमें पानी भी है या नहीं।
प्रयोक्ता के सम्मुख दूसरी समस्या सम्प्रेष्य वस्तु की है। यह बात
कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि काव्य का विषय और काव्य की
वस्तु (कंटेंट) अलग-अलग चीज़ें हैं; पर जान पड़ता है कि इस पर बल
देने की आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ती जाती है! यह बिलकुल सम्भव है कि हम
काव्य के लिए नये से नया विषय चुनें पर वस्तु उस की पुरानी ही रहे;
जैसे यह भी सम्भव है कि विषय पुराना रहे पर वस्तु नयी हो...
निस्सन्देह देश-काल की संक्रमणशील परिस्थितियों में संवेदनशील
व्यक्ति बहुत-कुछ नया देखे-सुने और अनुभव करेगा; और इसलिए विषय के
नयेपन के विचार का भी अपना स्थान है ही; पर विषय केवल नये हो सकते
हैं, मौलिक नहीं-मौलिकता वस्तु से ही सम्बन्ध रखती है। विषय
सम्प्रेष्य नहीं है, वस्तु सम्प्रेष्य है। नये (या पुराने भी) विषय
की, कवि की संवेदना पर प्रतिक्रिया, और उससे उत्पन्न सारे प्रभाव जो
पाठक-श्रोता-ग्राहक पर पड़ते हैं, और उन प्रभावों को सम्प्रेष्य
बनाने में कवि का योग (जो सम्पूर्ण चेतन भी हो सकता है, अंशत: चेतन
भी, और सम्पूर्णतया अवचेतन भी)- मौलिकता की कसौटी का यही क्षेत्र है।
यही कवि की शक्ति और प्रतिभा का भी क्षेत्र है-क्यों कि यही कवि मानस
की पहुँच और उसके सामथ्र्य का क्षेत्र है। कहाँ तक कवि नयी परिस्थिति
को स्वायत्त कर सका है (आयत्त करने में रागात्मक प्रतिक्रिया भी और
तज्जन्य बुद्धि-व्यापार भी है जिसके द्वारा कवि संवेदना का पुतला-भर
न बना रह कर उसे वश कर के, उसी के सहारे उससे ऊपर उठ कर उसे
सम्प्रेष्य बनाता है), इसी से हम निश्चय करते हैं कि वह कितना बड़ा
कवि है। [और फिर सम्प्रेषण के साधनों और तन्त्र (टेकनीक) के उपयोग की
पड़ताल कर के यह भी देख सकते हैं कि वह कितना सफल कवि है-पर इस पक्ष
को अभी छोड़ दिया जाय!]
यहाँ स्वीकार किया जाय कि नये कवियों में ऐसों की संख्या कम नहीं है
जिन्होंने विषय को वस्तु समझने की भूल की है, और इस प्रकार स्वयं भी
पथ-भ्रष्ट हुए हैं और पाठकों में नयी कविता के बारे में अनेक
भ्रान्तियों के कारण बने हैं।
लेकिन नकलचियों से सावधान! की चेतावनी असली माल वाले प्राय: नहीं
देते; या तो वे देते हैं जिन्हें स्वयं अपने माल की असलियत के बारे
में कुछ खटका हो, या फिर वे दे सकते हैं जो स्वयं माल लेकर उपस्थित
नहीं हैं और केवल पहरा दे रहे हैं। अर्थात् कवि स्वयं चेतावनी नहीं
देते; यह काम आलोचकों, अध्यापकों और संपादकों का है। यह भी उन्हीं का
काम है कि नकली के प्रति सावधान करते हुए असली की साख भी न बिगडऩे
दें- ऐसा न हो कि नकली से धोखा खाने के डर से सारा कारोबार ही ठप हो
जाय!
इस वर्ग ने यह काम नहीं किया है, यह सखेद स्वीकार करना होगा। बल्कि
कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि नकलची कवियों से कहीं अधिक संख्या और
अनुपात नकली आलोचकों का है-धातु उतना खोटा नहीं है जितनी कि कसौटियाँ
ही झूठी हैं! इतनी अधिक छोटी-मोटी एमेच्योर (और इम्मेच्योर)
साहित्य-पत्रिकाओं का निकलना, जब कि जो दो-चार सम्मान्य पत्रिकाएँ
हैं वे सामग्री की कमी से क्षयग्रस्त हो रही हैं, इसी बात का लक्षण
है कि यह वर्ग अपने कर्तव्य से कितना च्युत हुआ है। यह ठीक है कि ऐसे
छोटे-छोटे प्रयास एक आस्था की घोषणा करते हैं और इस प्रकार एक शक्ति
(चाहे कितनी स्वल्प) के लक्षण हैं, पर यह भी उतना ही सच है कि इस
प्रकार व्यापक, पुष्ट और दृढ़ आधार वाले मूल्यों की उपलब्धि और
प्रतिष्ठा का काम क्रमश: कठिनतर होता जाता है।
पर नकलची हर प्रवृत्ति के रहे हैं, और जिनका भंडाफोड़ अपने समय में
नहीं हुआ उन्हें पहचानने में फिर समय की दूरी अपेक्षित हुई है। अधिक
दूर न जावें तो न तो द्विवेदी युग में नकलचियों की कमी रही, न
छायावाद युग में। और न ही (यदि इसी सन्दर्भ में उन का उल्लेख भी उचित
हो जिन की उपलब्धि भी प्रयोगवादी सम्प्रदाय से विशेष अधिक नहीं रही
जान पड़ती) प्रगतिवाद ने कम नकलची पैदा किये। हमें किसी भी वर्ग में
उनका समर्थन या पक्ष-पोषण नहीं करना है-पर यह माँग भी करनी है कि
उनके अस्तित्व के कारण मूल्यवान् की उपेक्षा न हो, असली को नकली से न
मापा जाय।
शिल्प, तन्त्र या टेकनीक के बारे में भी दो शब्द कहना आवश्यक है। इन
नामों की इतनी चर्चा पहले नहीं होती थी। पर वह इसीलिए कि इन्हें एक
स्थान दे दिया गया था जिसके बारे में बहस नहीं हो सकती थी। यों साधना
की चर्चा होती थी, और साधना अभ्यास और मार्जन का ही दूसरा नाम था।
बड़ा कवि वाक्सिद्ध होता था, और भी बड़ा कवि रस सिद्ध होता था। आज
वाक्शिल्पी कहलाना अधिक गौरव की बात समझा जा सकता है-क्यों कि शिल्प
आज विवाद का विषय है। यह चर्चा उत्तर छायावाद काल से ही अधिक बढ़ी,
जब कि प्रगति के सम्प्रदाय ने शिल्प, रूप, तन्त्र आदि सब को गौण कह
कर एक ओर ठेल दिया, और शिल्पी एक प्रकार की गाली समझा जाने लगा। इसी
वर्ग ने नयी काव्य प्रवृत्ति को यह कह कर उड़ा देना चाहा है कि वह
केवल शिल्प का, रूप-विधान का आन्दोलन है, निरा फार्मेलिज़्म है। पर
साथ-साथ उसने यह भी पाया है कि शिल्प इतना नगण्य नहीं है; कि वस्तु
से रूपाकार को बिलकुल अलग किया ही नहीं जा सकता, कि दोनों का
सामंजस्य अधिक समर्थ और प्रभावशाली होता है; और इसी अनुभव के कारण
धीरे-धीरे वह भी मानो पिछवाड़े से आकर शिल्पाग्रही वर्ग में आ मिला
है। बल्कि अब यह भी कहा जाने लगा है कि प्रयोगवाद के जो विशिष्ट गुण
बताये जाते थे (जैसा बताने वाले वे ही थे!) उनका प्रयोगवाद ने ठेका
नहीं लिया है-प्रगतिवादी कवियों में भी वे पाये जाते हैं। इससे उलझी
परिस्थिति और भ्रामक हो गयी है। वास्तव में नयी कविता ने कभी अपने को
शिल्प तक सीमित रखना नहीं चाहा, न वैसी सीमा स्वीकार की। उस पर यह
आरोप उतना ही निराधार था जितना दूसरी ओर यह दावा कि केवल प्रगतिवादी
काव्य में सामाजिक चेतना है, और कहीं नहीं। यह मानने में कोई कठिनाई
न होनी चाहिए कि प्रगतिवाद सबसे अधिक समाजाग्रही रहा है; पर केवल इसी
से यह नहीं प्रमाणित हो जाता कि उस वाद के कवियों में गहरी सामाजिक
चेतना है या कि जैसी है वही उसका स्वस्थ रूप है-उसकी पड़ताल प्रत्येक
कवि में अलग करनी ही होगी।
खैर, यहाँ पुराने झगड़ों को
उठाना अभीष्ट नहीं है। कहना यह है कि नया कवि नयी वस्तु को ग्रहण और
प्रेषित करता हुआ शिल्प के प्रति कभी उदासीन नहीं रहा है, क्योंकि वह
उसे प्रेषण से काट कर अलग नहीं करता है। नयी शिल्प दृष्टि उसे मिली
है; यह दूसरी बात है कि वह सबमें एक-सी गहरी न हो, या सब देखे पथ पर
एक-सी सम गति से न चल सके हों। यहाँ फिर मूल्यांकन से पहले यह समझना
आवश्यक है कि यह नयी दृष्टि क्या है, और किधर चलने की प्रेरणा देती
है।
संकलित कवियों के विषय में अलग-अलग कुछ कहना कदाचित् उनके और पाठक के
बीच व्यर्थ एक पूर्वग्रह की दीवार खड़ी कर होगा। एक बार फिर इतना ही
कहना अलम् होगा कि ये कवि किसी एक सम्प्रदाय के नहीं हैं; न सबकी
साहित्यिक मान्यताएँ एक हैं, न सामाजिक, न राजनीतिक; न ही उनकी
जीवन-दृष्टि में ऐसी एकरूपता है। भाषा, छन्द, विषय, सामाजिक
प्रवृत्ति, राजनीतिक आग्रह या कर्म की दृष्टि से प्रत्येक की स्थिति
या दिशा अलग हो सकती है; कोई इस छोर के निकट पाया जा सकता है, कोई उस
छोर के, कोई बायें तो कोई दाहिने, कोई आगे तो कोई पीछे, कोई सशंक तो
कोई साहसिक। यह नहीं कि इन बातों का कोई मूल्य न हो। पर तीसरा सप्तक
में न तो ऐसा साम्य कलन का आधार बना है, न ऐसा वैषम्य बहिष्कार का।
संकलनकर्ता ने पहले भी इस बात को महत्त्व नहीं दिया है कि संकलित
कवियों के विचार कहाँ तक उसके विचारों से मिलते हैं या विरोधी है; न
अब वह इसे महत्त्व दे रहा है। क्योंकि उसका आग्रह रहा है कि काव्य के
आस्वादन के लिए इससे ऊपर उठ सकना चाहिए और उठना चाहिए। सप्तकों की
योजना का यही आधारभूत विश्वास है। प्रयोजनीय यह है कि संकलित कवियों
में अपने कवि-कर्म के प्रति गम्भीर उत्तरदायित्व का भाव हो, अपने
उद्देश्यों में निष्ठा और उन तक पहुँचने के साधनों के सदुपयोग की लगन
हो। जहाँ प्रयोग हो वहाँ कवि मानता हो कि वह सत्य का ही प्रयोग होना
चाहिए। यों काव्य में सत्य क्यों कि वस्तु सत्य का रागाश्रित रूप है
इसलिए उसमें व्यक्ति-वैचित्र्य की गुंजाइश तो है ही, बल्कि व्यक्ति
की छाप से युक्त होकर ही वह काव्य का सत्य हो सकता है। क्रीड़ा और
लीला-भाव भी सत्य हो सकते हैं-जीवन की ऋजुता भी उन्हें जन्म देती है
और संस्कारिता भी। देखना यह होता है कि यह सत्य के साथ खिलवाड़ या
फ्लर्टेशन मात्र न हो।
इन कवियों के एकत्र पाये जाने का आधार यही है। ऐसा दावा नहीं है कि
जिस काल या पीढ़ी के ये कवि हैं, उसके यही सर्वोत्कृष्ट या सबसे अधिक
उल्लेख्य कवि हैं। दो-एक और आमन्त्रित होकर भी इसलिए रह गये कि वे
स्वयं इसमें आना नहीं चाहते थे-चाहे इसलिए कि दूसरे कवियों का साथ
उन्हें पसन्द नहीं था, चाहे इसलिए कि संपादक का सम्पर्क उन्हें
अप्रीतिकर या हेय लगा, चाहे इसलिए कि वे अपने को पहले ही इतना
प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मानते थे कि नये कवियों के साथ आने में
उन्होंने अपनी हेठी या अपना अहित समझा। एक इसलिए रह गये कि उनकी
स्वीकृति के बावजूद दो वर्ष के परिश्रम के बार भी उनकी रचनाएँ न
प्राप्त हो सकीं। एक-दो इसलिए भी छोड़ दिये गये कि एकाधिक स्वतन्त्र
संग्रह प्रकाशित हो चुकने के कारण उनका ऐसे संकलन में आना अनावश्यक
हो गया था- स्मरण रहे कि मूल योजना यही थी कि सप्तक ऐसे कवियों को
सामने लाएँगे जिन जिनके स्वतन्त्र संग्रह प्रकाशित नहीं हुए हैं और
जो इस प्रकार भी नये हैं। यदि प्रस्तुत संकलन के भी दो-एक कवियों के
स्वतन्त्र संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं तो वह इसी बात का द्योतक है
कि तीसरा सप्तक की पांडुलिपि बनने और उसके प्रकाशन के बीच एक लम्बा
अन्तराल रहा है। यों हम तो चाहते हैं कि सभी कवियों के स्वतन्त्र
संग्रह छपें-बल्कि सप्तक में उन्हें लाने का कारण ही यह विश्वास है
कि उनके अपने-अपने संग्रह छपने चाहिए।
इन शब्दों के साथ हम ओट होते हैं। भूमिका का काम भूमि तैयार करना है;
भूमि तैयार वही है जिस पर चलने में उसकी ओर से बेखटके होकर उसे भुला
दिया जा सके। पाठक से अनुरोध है कि अब वह आगे बढ़ कर कवियों से
साक्षात्कार करे। उपलब्धि वहीं है।
दूसरों की रचनाओं के लिए
भूमिका लिखने का काम मुझे हमेशा कठिन जान पड़ा है। साधारणतया उसका
कारण यह होता है कि वह एक औपचारिक काम होता है। प्रस्तुत संकलन की
भूमिका औपचारिक काम तो नहीं है; चयन और संकलन स्वयं मैंने अपनी रुचि
और योजना के अनुसार किया है और यदि संकलित कवि मुझे महत्त्वपूर्ण लगे
हैं, उनकी रचनाएँ मुझे अच्छी लगी हैं तो उनके बारे में कुछ कहने में
औपचारिकता अनावश्यक है। इसके बावजूद भूमिका लिखने का काम अत्यन्त
दुष्कर जान पड़ रहा है। इसके कुछ कारण व्यक्तिगत हैं। फिर भी उनकी
चर्चा से बचना उचित अथवा संगत नहीं होगा क्योंकि उससे संपादक के
प्रति ही नहीं संकलित कवियों के प्रति भी अन्याय हो जाएगा।
पहले तीन सप्तकों के बाद यह चौथा सप्तक अपेक्षया लम्बे अन्तराल से
प्रकाशित हो रहा है। इस लम्बी अवधि में हिन्दी में कविता प्रचुर
मात्रा में लिखी गयी है। सब अच्छी नहीं है यह कहना किसी रहस्य का
उद्घाटन करना नहीं है। और शायद अगर यह भी कहूँ कि प्रकाशित कविता का
अधिकांश घटिया रहा है तो उसे पाठक एक अनावश्यक स्पष्टोक्ति भले ही
मान लें, गलत नहीं मानेंगे। किसी भी युग के काव्य के बारे में ऐसा ही
कहा जाता सकता है-अच्छा काव्य अनुपात की दृष्टि से थोड़ा ही रहता है।
लेकिन इस लम्बे अन्तराल की रचना में एक अंश छाँटना- सैकड़ों कवियों
में से केवल सात चुनना और फिर उनकी रचनाओं में से चयन करना-केवल
इसलिए कठिन नहीं है कि कवियों की बहुत बड़ी संख्या में से सात कवि
चुनने हैं। कठिनाई जितनी बाहर प्रस्तुत सामग्री में है उतनी ही चयन
करने वाले के आभ्यन्तर परिवर्तनों में और उनके कारण कवियों के बदले
हुए सम्बन्धों में भी है। निस्सन्देह प्रत्येक सप्तक के साथ यह
कठिनाई कुछ बढ़ती गयी। तार सप्तक का जब प्रकाशन हुआ तो उसमेंकलित
अन्य कवि सभी प्राय: मेरे समवयसी और साथी थे उनकी रचनाओं के चयन में
एक सहजता थी। उनके बारे में कुछ कहना भी इसी कारण कम कठिन था। जब
दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ तब भी परिस्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया
था, और तीसरा सप्तक में तो परिस्थिति स्पष्टत: बदली हुई थी। तार
सप्तक एक हद तक सहयोगी प्रकाशन था जिसे सहयोगियों ने एक न एक दिशा
देने के लिए संयोजित किया था; तीसरा सप्तक स्पष्टतया एक संपादक की
काव्य-दृष्टि और उसके काव्य-विवेक का प्रतिफलन था।
इतनी बात तो चौथा सप्तक के
बारे में भी सच है। और भी स्पष्ट कर के कहूँ कि यह घोषित रूप से, एक
संपादक की काव्य दृष्टि, साहित्यिक रुचि और साहित्यिक विवेक का
प्रतिफलन है। लेकिन तीसरा सप्तक के समय की अपेक्षा आज यह काम कितना
कठिनतर हो गया इसकी ओर पाठक का ध्यान दिलाना आवश्यक है। शायद उस
कठिनाई को स्पष्ट कर देने का सबसे अच्छा तरीका यही हो कि मैं यह
स्वीकार करूँ कि पहले तीन सप्तकों का संपादन करते हुए मैं यह अनुभव
करता रहा था कि मैं काव्य में कुछ ऐसी नयी प्रवृत्तियों का
व्याख्याता और वकील हूँ, जिनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। अर्थात्
पहले तीन सप्तक मेरी दृष्टि में एक तरह के साहित्यिक आन्दोलन और
युग-परिवर्तन के अंग थे। तीसरा सप्तक के बाद मुझे ऐसा जाना पड़ा कि
वे नयी प्रवृत्तियाँ काव्यप्रेमी समाज में पूरी तरह स्वीकृति पा गयी
हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए और आन्दोलन अथवा वकालत की कोई आवश्यकता
नहीं रही। और मन ही मन मैं इस परिणाम पर भी पहुँच चुका था कि अब
सप्तकों के क्रम में और कोई संकलन जोडऩा अनावश्यक हो गया है। बल्कि
उसके बाद के कुछ वर्षों में तो ऐसा अनुभव हुआ कि स्वीकार की
प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ गयी है कि नयी रचनाओं का दोष देखना भी कठिन
हो गया है : उस धारा में बह कर आने वाला सभी कुछ स्वीकार कर लिया
जाता है और यहाँ तक कि पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों को अपने विवेक से
काम लेते डर लगता है! मैंने कहा कि किसी भी युग का समूचा
काव्य-साहित्य समान रूप से अच्छा नहीं होता; कुछ अच्छी रचनाओं के साथ
बहुत ही साधारण कोटि की या उससे भी निचले स्तर की रचनाएँ प्रकाश में
आती रहती हैं। जिस स्थिति में पत्रिकाओं की बाढ़ हो और उसके साथ-साथ
प्रतिमान सामने रखने वाली कोई सर्वमान्य पत्रिका न हो, साधारण और
घटिया रचनाओं का प्रसार और भी बढ़ जाता है। लेकिन यह मान लेने के साथ
इस बात का उल्लेख भी आवश्यक है कि तार सप्तक के संपादक को तीसरा
सप्तक के बाद के युग की स्थिति से कुछ अतिरिक्त क्लेश इसलिए भी होने
लगा कि वय के अन्तर के साथ संवेदन का अन्तर भी स्वभावत: बढऩे लगा।
मैं नहीं जानता कि तार सप्तक के जो कवि आज जीवित हैं वे सभी इस बात
को स्वीकार करेंगे या नहीं; लेकिन उन के स्वीकार न करने पर भी मैं तो
यही मानूँगा कि यह बात उनके बारे में भी उतनी ही सच होगी।
ऐसी बढ़ती हुई दूरी अनिवार्य है और उसके साथ-साथ इच्छा रहते भी
समानता का कठिनतर होते जाना भी स्वाभाविक है। इससे एक परिणाम तो यह
निकलता ही है कि आज जो कविता लिखी जा रही है उसे अगर एक मुकदमे के
रूप में प्रस्तुत करना है तो उसका वकील उसी में से निकलना चाहिए-आज
जो लिखा जा रहा है उसका सच्चा वकील आज का लिखने वाला ही होना चाहिए।
वैसे संकलन प्रकाशित होते भी रहे हैं, अभी हाल में दो-तीन हुए हैं।
मुकदमे का विचार जिन्हें करना हो उन्हें अवश्य ही वे संग्रह देखने
चाहिए और उनकी भूमिकाओं में अथवा कवियों के वक्तव्यों में दी गयी
दलीलों का विचार करना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं उस दरजे का वकील नहीं
हो सकता तो इसमें एक अनिवार्यता है जिसे मैंन केवल स्वीकार करना
चाहता हूँ बल्कि जिसकी ओर पाठक का ध्यान भी दिला देना चाहता हूँ।
क्योंकि यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि चौथा सप्तक में जिन कवियों
की रचनाएँ मैं चुन कर प्रस्तुत कर रहा हूँ उन का मैं प्रशंसक तो
अवश्य हूँ, लेकिन उन्हें पाठक के सामने प्रस्तुत करते हुए उनके साथ
एक दूरी, एक तटस्थता का भी बोध मुझमें है। मैं उन प्रशंसक हॅँ, मैं
उनमें से एक नहीं हूँ-या हूँ तो उसी अर्थ में जिस अर्थ में किसी भी
युग का कोई भी कवि किसी दूसरे युग के कवि के साथ होता है। कवियों की
बिरादरी में भी किसी भी दूसरी बिरादरी की तरह एक बन्धन समकालीनता का
होता है तो एक अनुक्रमिकता का। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी इस लाचारी
का दंड संकलित कवियों को मिले। इस मामले में मेरी सतर्कता और बढ़
जाती है क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनका जोखिम अधिक है। तीसरा सप्तक
के बाद के लम्बे अन्तराल का एक परिणाम यह भी हुआ है कि चौथा सप्तक
में रखे गये कवियों के बीच वयस की दृष्टि से काफ़ी अन्तर है। यह तो
सम्भव था कि इससे बचने के लिए सभी कवि युवतर वर्ग में से चुने जाते;
लेकिन उससे भी एक दूसरे प्रकार का अन्याय हो जाता-केवल बीच की पीढ़ी
के छूट जाने वाले कवियों के प्रति नहीं बल्कि संकलित कवियों के प्रति
भी, इसलिए कि पाठक उनकी रचनाओं का मूल्यांकन करते हुए उन कवियों को
भी सामने रखता तो बीच के अन्तराल के प्रमुख कवि थे। यों तो अब भी यह
सम्भावना बनी ही रहेगी क्यों कि सात की संख्या को सीमा बना लेने से
कई कवि छूट जाते हैं। लेकिन यह बात तो पाठक बहुत आसानी से समझ
सकेंगे।
पाठक को एक और बात याद दिला देना उचित होगा। कवियों का चयन करते समय
एक बात यह भी मेरे ध्यान में थी कि जिन कवियों के एक से अधिक
स्वतन्त्र संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं उन्हें छोड़ भी दिया जा सकता
है क्यों कि वे तो पाठक के सामने मौजूद हैं। मुझे यह प्रयत्न करना
चाहिए कि जो अच्छे रचनाकार सभी अपेक्षया कम प्रसिद्ध हुए हैं उन्हें
सामने लाया जाये। चौथा सप्तक के संकलित कवियों में से दो-तीन की
रचनाएँ पुस्तकाकार छप चुकी थीं, लेकिन कारण चाहे जो रहा हो
काव्यप्रेमी जनता के सामने नहीं आ सकी थीं। यह भी सम्भव है कि चयन की
प्रक्रिया आरम्भ होने से लेकर इस पुस्तक के प्रकाशन तक की अवधि में
संगृहीत और भी दो-एक कवियों के एकल संग्रह प्रकाशित हो जाएँ। मैं
नहीं समझता कि उससे मेरा प्रयत्न दूषित होगा। मुझे तो प्रसन्नता होगी
कि जिन कवियों को मैं उल्लेख्य मानता हूँ उनके नये स्वतन्त्र संग्रह
सामने आ रहे हैं।
(2)
मैं कह आया कि तीन सप्तकों
के प्रकाशन से मुझे वह प्रक्रिया पूरी हो गयी जान पड़ी थी जो नयी
काव्य-प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक थी। मैंने यह भी कहा
कि उसके बाद कभी-कभी ऐसा भी अनुभव हुआ कि गुण-दोष-विवेक अपना आधार खो
बैठा है। ऐसा लगने लगा कि एक पक्ष की वकालत कर चुकने के बाद अब
प्रतिपक्ष की ओर से भी कुछ कहना आवश्यक हो गया है। लेकिन कविता के
प्रतिपक्ष का मेरे लिए तो कुछ अर्थ नहीं है-मैं सदैव सत्काव्य का
समर्थक हूँ और बना रहना चाहूँगा। समकालीन काव्य के दोषों अथवा उसकी
त्रुटियों का उल्लेख करूँगा तो प्रतिपक्षी भाव से नहीं, वरन् उसके
श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने लाने के लिए ही। और उसमें यह भी कहना उचित
होगा कि काव्य के गुण-दोष की ओर ध्यान दिलाते हुए समकालीन आलोचना की
त्रुटियों और उसकी एकांगिता को भी अनदेखा न करना होगा। इस एकांगिता
ने नयी रचना का बहुत अहित किया है। उसने नये रचनाकार को दिग्भ्रमित
किया है और पाठक को भी इसलिए पथभ्रष्ट किया है कि उसने पाठक के सामने
जो कसौटियाँ दी हैं वे स्वयं झूठी हैं। नयी कविता ने एक बार फिर
रचयिता और गृहीता समाज का सम्बन्ध स्थापित किया था, संचार की
प्रणलियाँ बनायी थीं और खोली थीं। संकीर्ण और मताग्रही आलोचना ने फिर
उन्हें अवरुद्ध कर दिया है। कवियों की संख्या कम नहीं हुई-हो सकता है
कि कुछ बढ़ ही गयी हो-लेकिन कवि समुदाय पाठक अथवा श्रोता समाज के न
केवल निकटतर नहीं आया है बल्कि उस समाज में उसने फिर एक उदासीनता का
भाव पैदा कर दिया है। इसके कारणों की कुछ पड़ताल अपेक्षित है।
यह तो कहा जा सकता है कि आज की कविता में जो प्रवृत्तियाँ मुखर हुई
हैं उन के बीज उससे पहले की कविता में मौजूद थे-उस कविता में भी जिसे
प्रयोगवादी कहा जाता है और उसमें भी जिसे प्रगतिवादी नाम दिया जाता
है। (दोनों ही नाम गलत हैं, लेकिन उस बहस में अभी न पड़ा जाए।) यह
बात वैसे ही सही होगी जैसे यह बात कि प्रयोगवादी अथवा प्रगतिवादी
प्रवृत्तियों के बीज छायावादियों में थे और छायावाद के बाद उससे पहले
के इतिवृत्तात्मक काव्य में इत्यादि। ऐसा तो होता ही है क्यों कि
कविता कविता में से ही निकलती है, लेकिन इसके कारण हम किसी एक युग
अथवा धारा अथवा आन्दोलन की प्रवृत्तियों के गुण-दोष का विवेचन करते
समय सारी जिम्मेदारी उसके पूर्ववर्तियों पर नहीं थोप देते। किसी भी
युग के आग्रह उसी युग के होते हैं और उनकी जिम्मेदारी उसी पर होती
है।
आज की कविता में वक्तव्य का प्राधान्य हो गया है। उसके भीतर जो
आन्दोलन हुए हैं और हो रहे हैं वे सभी इस बात को न केवल स्वीकार करते
हैं बल्कि बहुधा इसी को अपने दावे का आधार बनाते हैं। कविता में
वक्तव्य तो हो सकता है और वक्तव्य होने से ही वह अग्राह्य हो जाए ऐसा
भी नहीं है। लेकिन वक्तव्य के भी नियम होते हैं और उनकी अपेक्षा
काव्य के लिए खतरनाक होती है। यह बात उतनी ही सच है जितनी यह कि
काव्य में कवि वक्ता के रूप में भी आ सकता है, लेकिन उत्तम पुरुष के
प्रयोग की जो मर्यादाएँ हैं उनकी अपेक्षा करने से कविता का मैं कवि न
होकर एक अनधिकारी आक्रान्ता ही हो जाता है। आज कविता पर एक दावे करने
वाला मैं बुरी तरह छा गया है। कविता में मैं भी निषिद्ध नहीं है,
दावे भी निषिद्ध नहीं हैं, कविता प्रतिश्रुत और प्रतिबद्ध भी हो सकती
है, लेकिन कहाँ अथवा कहाँ तक इन सबका काव्य में निर्वाह हो सकता है
और कहाँ ये काव्य के शत्रु बन जाते हैं यह समझना आवश्यक है।
मंच पर हम नाटक देखते हैं तो उसमें आने वाला प्रत्येक चरित्र वक्ता
होता है, उत्तम पुरुष में अपना वक्तव्य देता है, प्रतिश्रुत और
प्रतिबद्ध होता है; हमारे सामने अभिनेता होता है, लेकिन हम देखते हैं
तो अभिनेता को नहीं, उसके माध्यम से प्रस्तुत होते हुए चरित्र को। हम
यह कभी नहीं भूलते कि हमारे सामने एक अभिनेता है, लेकिन फिर भी देखते
हैं हम चरित्र को ही। अभिनेता कहता है मैं लेकिन वह मैं हमारे लिए
चरित्र के वक्तव्य का स्वर होता है। ऐसी स्थिति में नाटक के डायलाग
अत्यन्त काव्यमय भी हो सकते हैं। लेकिन उन्हीं शब्दों में वही
वक्तव्य यदि अभिनेता द्वारा प्रस्तुत किये गये चरित्र का न होकर
स्वयं अभिनेता का होता, मंच पर बोलने वाला मैं यदि वह चरित्र न होता
जो होकर भी वहाँ नहीं है, उसके बदले में स्वयं अभिनेता होता तो
बिलकुल $ज़रूरी नहीं है कि वही वक्तव्य उस स्थिति में भी हमें
काव्यमय जान पड़ता या हमें सहन भी होता। अभिनेता द्वारा प्रस्तुत
किये गये चरित्र को हम अपना वक्तव्य उत्तर पुरुष एक वचन में देने का
अधिकार देते हैं; अभिनेता को वह अधिकार हम नहीं देते, यानी एक चेहरा,
मास्क और पर्सोना हमें स्वीकार है, स्वयं नट हमें स्वीकार नहीं है।
वाक्य में इस बात का महत्त्व है। संस्कृत में काव्य का एक दृश्य रूप
था और एक श्रव्य; काव्य दोनों ही थे। और पर्सोना अथवा अभिनेय चरित्र
के साथ सम्बन्ध दृश्य काव्य में ही नहीं, श्रव्य काव्य में भी अपना
महत्त्व रखता है। काव्य में बोलने वाला हर मैं पर्सोना होता है,
अभिनेय चरित्र होता है। जब कवि स्वयं अपनी बात भी कहता है तो वह हमें
तभी स्वीकार होती है-मैं कह सकता हूँ कि तभी सह्य भी होती है-जब वह
कथ्य अथवा वक्तव्य प्रत्यक्ष रूप से कवि का न होकर एक पर्सोना अथवा
अभिनेय चरित्र के रूप में उसका हो।
और इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात को आज की कविता के अधिसंख्य कवि भूल
गये हैं और विस्मृति में आज के आलोचक ने उनकी सहायता की है। मास्क
अथवा चेहरे अथवा मुखौटे के प्रति जिस अवज्ञा भाव को इतना बढ़ावा दिया
गया है उसने यह भी भुला देने में हमारी मदद की है कि मुखौटे केवल
धोखा देने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को प्रस्तुत करने के लिए भी
लगाये जाते हैं। साधारण जीवन में मुखौटा फ़रेब है, लेकिन नाटक में वही
मुखौटा एक वृहत्तर यथार्थ में हमें लौटा लाने में सहायक हो सकता है-
ऐसे वृहत्तर यथार्थ में जिसका सामना शायद हम बिना मुखौटे के कर ही न
सकें। सारे संसार के नाट्य से हम इस बात का प्रमाण पा सकते हैं-जहाँ
भी साधारण सच्चाइयों से आगे बढ़ कर विराट् को स्थापित करने का
प्रयत्न होता है, वहाँ मुखौटे आते हैं।
कविता के लिए-काव्य के श्रव्य रूप के लिए-इस बात का क्या महत्त्व है?
यही कि वक्तव्य वक्तव्य होने के नाते अग्राह्य नहीं है, तब अग्राह्य
हो जाता है जब उसमें केवल कवि-रूपी इकाई का मैं अथवा अहम् बोलता है।
अग्राह्य नहीं तो महत्त्वहीन तो वह हो ही जाता है क्यों कि हमारा
प्रयोजन कविता से है, कवि से नहीं, या कवि से है तो बिलकुल
साधारण-सा।
और हर युग के महान् कवि इस
बात को पहचानते रहे हैं। यह नहीं है कि कवियों ने अपनी भावनाएँ, अपने
राग-विराग, अपनी लालसाएँ और आकांक्षाएँ व्यक्त नहीं कीं, लेकिन जब की
हैं और काव्य रूप में की है तो किसी दूसरे चरित्र पर उनका आरोप करके।
भक्त कवियों ने प्रेम अथवा विरह की जिन अवस्थाओं का वर्णन कृष्ण और
राधा अथवा गोपियों के माध्यम से इतने मार्मिक ढंग से किया है, ऐसा
नहीं है कि उन भावनाओं से वे अपने जीवन में अपरिचित रहे होंगे, लेकिन
उन्हीं भावनाओं को वे अपनी, कवि की निजी, भावनाओं के रूप में
प्रस्तुत करते तो वे न केवल श्रेष्ठ काव्य की कोटि में न आतीं वरन्
असमंजस का कारण भी बनतीं-लगभग अश्लील जान पडऩे लगतीं। और भक्त कवियों
तक ही क्यों सीमित रहें-कोई कह सकता है कि भक्ति की बात तो लौकिक और
अलौकिक के बीच के सम्बन्ध की है-शुद्ध लौकिक स्तर पर रह कर हम रीति
के कवियों का भी उदाहरण लें : वहाँ भी मैं कभी नहीं आता, नायक अथवा
नायिका आती है, यद्यपि उन पर आरोपित भावनाएँ बिलकुल मानवीय हैं और
माना जा सकता है कि कवि अथवा कवयित्री के निजी जीवनानुभव से सम्बद्ध
रही हैं। वक्तव्य वहाँ है निजी और अन्तरंग, ऐसे भावों की
अभिव्यक्तिभी है जो साधारण जीवन में सामने आने पर असमंजस का,
अस्वस्ति भाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन रीति काव्य के छन्दों में
क्यों वे इतने ग्राह्य, इतने आकर्षक, इतने मार्मिक हो जाते हैं?
क्यों कि वहाँ कवि मैं के रूप में आपके सामने नहीं आता। वह यह दावा
नहीं करता कि यह मेरा भोगा हुआ यथार्थ है। भोगा हुआ तो वह अवश्य है,
लेकिन जिसका भोगा हुआ है वह दावेदार बन कर आपके सामने नहीं आता, वह
उसे एक-दूसरे को सौंप देता है।
इस सौंप देने का एक विशेष महत्त्व हैं। यह सौंप दे सकना अपने-आप में
साधारणीकरण की एक कसौटी है। कवि जहाँ मैं के रूप में पाठक अथवा
श्रोता के समक्ष होकर अपना वक्तव्य देता है वहाँ इस बात की कोई
गारंटी नहीं है कि वह वक्तव्य या उसमें प्रकट किये गये भाव अथवा
विचार एक सार्वभौम सत्ता पा चुके हैं। दूसरे शब्दों में यह सिद्ध
नहीं हुआ है कि वे बहुजन-संवेद्य हो गये हैं, सम्प्रेष्य हो गये हैं।
उन्हीं को जब हम दूसरे चरित्र के माध्यम से-नायक अथवा नायिका अथवा
पर्सोना के माध्यम से-प्रस्तुत करते हैं, तब इस कसौटी पर हम अपनी
परीक्षा करवा चुके होते हैं।
तो एक बार अपनी बात मैं दोहरा दूँ। आज की कविता का बहुत बड़ा और शायद
सबसे बड़ा दोष यह है कि उस पर एक ‘मैं’ छा गया है, वह भी एक
अपरीक्षित और अविसर्जित मैं। आज की कविता बहुत बोलती है, जब कि कविता
का काम बोलना है ही नहीं।
(3)
यदि यह कहा जाए कि आज कवि के
पास सामान्यतया पिछली पीढ़ी के कवि से अधिक जानकारी होती है और वह
साधारण जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में
अधिक सजग और सतर्क होता है तो इसे कोई आश्चर्यजनक स्थापना नहीं समझा
जाएगा क्योंकि यह समूचे समाज के विकास की दिशा के अनुरूप ही है, और
यदि इस व्यापकतर व्यावहारिक जागरूकता का एक पहलू राजनीतिक जागरूकता
है तो वह भी स्वाभाविक है क्योंकि व्यावहारिक जीवन में राजनीति का
स्थान और महत्त्व लगातार बढ़ता गया है। लेकिन जो बात चिन्त्य है वह
यह कि कवि की राजनीतिक चेतना के साथ राजनीतिक मतवाद का आरोप कहाँ तक
उचित है? क्या कविता को अनिवार्यतया किसी राजनीतिक सन्देश की वाहिका
होना चाहिए? और जो कविता संकल्पपूर्वक किसी राजनीतिक मत का प्रतिपादन
करने नहीं चलती वह क्या इसीलिए अनिवार्यतया घटिया हो जाएगी? क्या
काव्य केवल एक साधन है?
सप्तकों की परम्परा में कभी इस बात को आवश्यकता से अधिक महत्त्व नहीं
दिया गया कि संकलित कवियों के राजनीतिक विचार क्या हैं। राजनीतिक
पक्षधरता को कभी कसौटी नहीं बनाया गया। चौथा सप्तक में भी उस कसौटी
से काम नहीं लिया गया है और पाठक जानेंगे-जैसा कि संपादक भी जानता
है-कि संकलित कवियों के राजनीतिक विचार और उनके राजनीतिक सम्पर्क
अथवा आस्थाएँ बिलकुल अलग-अलग हैं। लेकिन इस बात पर बल देकर इस ओर भी
ध्यान देना चाहिए कि आज का राजनीतिक और साहित्यिक वातावरण पहले से
बहुत बदला हुआ है और राजनीति में मतवादों के साथ-साथ साहित्य में
मतवादी चिन्ता का दावा बढ़ता गया है। शायद राजनीति में भी उसके कुछ
दुष्परिणाम हुए हैं, लेकिन उनकी चर्चा को विषयान्तर मान कर छोड़ दें
तो यह कहना होगा कि मतवादी साहित्य-चिन्तन ने काव्य का अहित ही किया
है। साहित्य और राजनीति के सम्बन्धों की चर्चा तो पचास वर्ष पहले
शुरू की गयी थी, लेकिन अपने प्रारम्भिक दिनों में प्रगतिशीलता का
आन्दोलन उन सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयत्न कर रहा था जिनके
विचारों को साधारण तौर पर प्रगतिशील कहा जा सके। उस दौर के कवियों को
भी नये चिन्तन से प्रेरणा मिली और उनकी काव्य-रचना ने भी राजनीतिक
आन्दोलन को बल दिया। उसके बाद कैसे बढ़ती हुई वैचारिक संकीर्णता और
असहिष्णुता के कारण प्राय: सभी बड़े साहित्यकार एक-एक कर के निकाल
दिये गये या स्वयं अलग हट गये और इसमेंसे कैसे आन्दोलन ही मृतप्राय
हो गया, ये बातें समकालीन साहित्य के इतिहास का अंग हो गयी हैं। जिस
काल की रचनाओं से चौथा सप्तक के कवि और उनकी कविताएँ ली गयी हैं
उसमें फिर राजनीतिक पक्षधरता के आन्दोलन एक से अधिक दिशाओं में आरम्भ
हुए और ध्रुवीकरण के नाम पर फिर एक व्यापक असहिष्णुता का वातावरण बन
गया। आपातकाल ने एक लगभग देशव्यापी आतंक की सृष्टि की तो उसकी परिधि
के भीतर विभिन्न प्रकार की असहिष्णुताएँ आतंक के छोटे-छोटे मंडल
बनाती रहीं। आपातकाल की समाप्ति से आतंक का तो अन्त हो गया, लेकिन
मतवादी असहिष्णुताओं के ये वृत्त अभी कायम हैं। चौथा सप्तक के सभी
कवि इस परिस्थिति से न केवल परिचित रहे हैं बल्कि उसके दबाव का तीखा
अनुभव भी करते रहे हैं और कुछ ने उसके कारण कष्ट भी सहा है। इसलिए
अगर मैं कहूँ कि संकलित कवियों के राजनीतिक विचारों के अलग होते हुए
भी एक स्तर पर वे एक सामान्य अनुभव की बिरादरी में आ जाते हैं तो यह
कथन अनुचित न होगा और वह सामान्य अनुभव है एक स्वातंत्र्य का अनुभव।
कवि के संसार की स्वायत्तता का एक बोध संकलित सभी कवियों की रचनाओं
में मिलता है- कुछ में अधिक परिपक्व तो कुछ में कम, लेकिन सर्वत्र
काव्य के स्वर में अपनी एक विशेष गूँज मिलाए हुए। यह कदाचित चौथा
सप्तक के कवियों का-और उनके युग की अच्छी कविता का-विशेष गुण है। और
आशा की जा सकती है कि एक सार्वभौम मौलिक मूल्य के इस आग्रह के कारण
चौथा सप्तक की कविताएँ न केवल स्वयं लोकप्रिय हो सकेंगी वरन् कविता
के प्रति जिस उदासीनता की बात मैंने पहले की है उसे भी कुछ कम कर
सकेंगी।
(4)
मैं नहीं जानता कि संकलित
सातों कवियों के बारे में अलग-अलग कोई समीक्षात्मक टिप्पणी अथवा
संस्तुति मुझसे अपेक्षित है या नहीं। लेकिन अपेक्षित हो भी तो वह काम
मैं अभी नहीं करने जा रहा हूँ। यों भी यही उचित है कि पाठक इन कवियों
से साक्षात्कार करते समय और उनके काव्य-संसार में प्रवेश करते समय
मेरे पूर्वग्रहों का बोझ न लेकर चले, मेरे चश्मे से न देखे। इसके
अलावा मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरी संस्तुतियों की प्रतिकूल
प्रतिक्रिया का दंड इन कवियों को मिले-और मैं कटु अनुभव से जानता हूँ
कि ऐसा प्राय: होता आया है! निश्चय ही जिस पीढ़ी या जिन दशकों से ये
कवि चुने गये हैं उनमें और भी अच्छी रचनाएँ हुई हैं, पर उनका अथवा
उनके कवियों का यहाँ न पाया जाना इस बात का द्योतक नहीं है कि मैं
उनकी अवमानना करना चाहता हूँ। मेरा दावा इतना ही होगा कि संकलित कवि
इस अवधि की अच्छी कविता का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि उनकी रचनाएँ
किसी बिन्दु पर आकर ठहर नहीं गयी हैं, बल्कि उनकी काव्य-प्रतिभा का
अभी और विकास हो रहा है, कि इसीलिए मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य
में इन कवियों के कृतित्व की छाप समकालीन हिन्दी काव्य पर और गहरी
पड़ेगी।
और यह बात संकलित कवियों के प्रति मेरी शुभाशंसा भी है, चौथा सप्तक
के पाठक को मेरा आश्वासन भी।
प्रकृति की चर्चा करते समय
सबसे पहले परिभाषा का प्रश्र उठ खड़ा होता है। प्रकृति हम कहते किसे
हैं? वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर एक प्रकार से देते हैं, दार्शनिक
दूसरे प्रकार से, धर्म-तत्त्व के चिन्तक एक तीसरे ही प्रकार से। और
हम चाहें तो इतना और जोड़ दे सकते हैं कि साधारण-व्यक्ति का उत्तर इन
सभी से भिन्न प्रकार का होता है।
और जब हम ‘एक प्रकार का उत्तर’ कहते हैं, तब उसका अभिप्राय एक उत्तर
नहीं है, क्योंकि एक ही प्रकार के अनेक उत्तर हो सकते हैं। इसीलिए
वैज्ञानिक उत्तर भी अनेक होते हैं; दार्शनिक उत्तर तो अनेक होंगे ही,
और धर्म पर आधारित उत्तरों की संख्या धर्मों की संख्या से कम क्यों
होने लगी?
प्रश्न को हम केवल साहित्य के प्रसंग में देखें तो कदाचित् इन
अलग-अलग प्रकार के उत्तरों को एक सन्दर्भ दिया जा सकता है।
साहित्यकार की दृष्टि ही इन विभिन्न दृष्टियों के परस्पर विरोधों से
ऊपर उठ सकती है- उन सबको स्वीकार करती हुई भी सामंजस्य पा सकती है।
किन्तु साहित्यिक दृष्टि की अपनी समस्याएँ हैं; क्योंकि एक तो
साहित्य दर्शन, विज्ञान और धर्म के विश्वासों से परे नहीं होता,
दूसरे सांस्कृतिक परिस्थितियों के विकास के साथ-साथ साहित्यिक
संवेदना के रूप भी बदलते रहते हैं।
साधारण बोलचाल में ‘प्रकृति’ ‘मानव’ का प्रतिपक्ष है, अर्थात मानवेतर
ही प्रकृति है-वह सम्पूर्ण परिवेश जिसमें मानव रहता है, जीता है,
भोगता है और संस्कार ग्रहण करता है। और भी स्थूल दृष्टि से देखने पर
प्रकृति मानवेतर का वह अंश हो जाती है जो कि इन्द्रियगोचर है-जिसे हम
देख, सुन और छू सकते हैं, जिसकी गन्ध पा सकते हैं और जिसका आस्वादन
कर सकते हैं। साहित्य की दृष्टि कहीं भी इस स्थूल परिभाषा का खंडन
नहीं करती : किन्तु साथ ही कभी अपने को इसी तक सीमित भी नहीं रखती।
अथवा यों कहें कि अपनी स्वस्थ अवस्था में साहित्य का प्रकृति-बोध
मानवेतर, इन्द्रियगोचर, बाह्य परिवेश तक जाकर ही नहीं रुक जाता;
क्योंकि साहित्यिक आन्दोलनों की अधोगति में विकृति की ऐसी अवस्थाएँ
आती रही हैं जब उसने बाह्य सौन्दर्य के तत्त्वों के परिगणन को ही
दृष्टि की इति मान लिया है। यह साहित्य की अन्त:शक्ति का ही प्रमाण
है कि ऐसी रुग्ण अवस्था से वह फिर अपने को मुक्त कर ले सका है, और न
केवल आभ्यन्तर की ओर उन्मुख हुआ है बल्कि नयी और व्यापकतर संवेदना
पाकर उस आभ्यन्तर के साथ नया राग-सम्बन्ध भी जोड़ सका है।
राग-सम्बन्ध अनिवार्यतया
साहित्य का क्षेत्र है। किन्तु राग-सम्बन्ध उतने ही अनिवार्य रूप से
साहित्यकार की दार्शनिक पीठिका पर निर्भर करते हैं। यदि हम मानते
हैं-जैसा कि कुछ दर्शन मानते रहे-कि प्रकृति सत् है, मूलत: कल्याणमय
है, तब उसके साथ हमारा राग-सम्बन्ध एक प्रकार का होगा-अथवा हम
चाहेंगे कि एक प्रकार का हो। यदि हम मानते हैं कि प्रकृति मूलत: असत्
है, तो स्पष्ट ही हमारी राग-वृत्ति की दिशा दूसरी होगी। यदि हम मानते
हैं कि प्रकृति त्रिगुण-मय है किन्तु अविवेकी है, तो हमारी प्रवृत्ति
और होगी : और यदि हमारी धारणा है कि प्रकृति सदसद् से परे है तो हम
उसके साथ दूसरे ही प्रकार का राग-सम्बन्ध चाहेंगे-अथवा कदाचित् यही
चाहेंगे कि जहाँ तक प्रकृति का सम्बन्ध है हम वीतराग हो जाएँ!
विभिन्न युगों के साहित्यकारों के प्रकृति के प्रति भाव की पड़ताल
करने में हम उन भावों में और साहित्यकार के प्रकृति-दर्शन में स्पष्ट
सम्बन्ध देख सकेंगे।
कवियों के प्रकृति-वर्णन
अथवा निरूपण की चर्चा में उनके आधारभूत दार्शनिक विचारों अथवा
धर्म-विश्वासों तक जाना यहाँ कदाचित अनपेक्षित होगा। उतने विस्तार के
लिए यहाँ स्थान भी नहीं है। किन्तु कवि के संवेदन पर उसकी दार्शनिक
अथवा धार्मिक आस्था के प्रभाव की अनिवार्यता को स्वीकार करके हम
प्रकृति-वर्णन की परम्परा का अध्ययन कर सकते हैं। वैदिक
कवि-मन्त्रद्रष्टा को कवि कहना उसकी अवहेलना नहीं है-प्रकृति की
सत्ता का सम्मान करता था और मानता था कि उसकी अनुकूलता ही सुख और
समृद्धि का आधार है। सुखी और सम्पूर्ण जीवन का जो चित्र उसके सम्मुख
था उसमें मनुष्य की और प्रकृति की शक्तियों की परस्पर अनुकूलता
आवश्यक थी। प्राकृतिक शक्तियों को वह देवता मानता था, किन्तु देवता
होने से ही वे अनुकूल हो जाएँगी ऐसा उसका विश्वास नहीं था-उनकी
अनुकूलता के लिए वह प्रार्थी था। कहा जा सकता है कि उसकी दृष्टि में
ये शक्तियाँ सदसद् से परे ही थीं किन्तु उन्हें अनुकूल बनाया जा सकता
था।
यथा द्यौश्च पृथ्वी च न
विभीतो न रिष्यत :
एवा मे प्राण मा बिभै :
यथाऽहश्च रात्री च न विभीतो न रिष्यत:
एवा मे प्राण मा बिभै:
यह प्रार्थना करने वाला
व्यक्ति जहाँ यह कामना करता था कि प्रकृति की शक्तियों के प्रति उसके
प्राण भय रहित हों, वहाँ यह भी मानता था कि वे शक्तियाँ भी राग-द्वेष
से परे हैं। इतना ही नहीं, मध्य युग की पाप-पुण्य की भावना भी उसमें
नहीं थी-हो भी नहीं सकती थी जब तक कि वह प्रकृति को पापमूलक न मान
लेता-और उसके निकट दिन और रात, प्रकाश और अन्धकार, सत्य और असत्य,
सभी एक से निर्भय थे। वह अपनी प्रार्थना में यह भी कहता था कि-
यथा सत्यं चाऽनृतं च न
विभीतो न रिष्यत:
एवा मे प्राण मा बिभै: ॥
यह कहने का साहस मध्य काल के
कवि को नहीं हो सकता था-पाप की परिकल्पना कर लेने के बाद यह सम्भावना
ही सामने नहीं आती कि अनृत भी सत्य के समान ही निर्भय हो सकता है।
वैदिक कवि क्योंकि प्रकृति को न सत् मानता है न असत्, इसलिए प्रकृति
के प्रति उसका भाव न प्रेम का है न विरोध का। वह मूलत: एक विस्मय का
भाव है।
हिरण्यगर्भ:
समवर्तताग्रे
यह उसके भव्य विस्मय की ही
उक्ति है। और यदि वह आगे पूछता है-
कस्मै देवाय हविषा
विधेम?
तो यह किंकर्तव्यता भी आतंक
का नहीं, शुद्ध विस्मय का ही प्रतिबिम्ब है। उषा-सूक्त में उषा के
रूप का वर्णन, पृथ्वी-सूक्त में पृथ्वी से पृथ्वी-पुत्र मनुष्य के
सम्बन्ध का निरूपण, इन्द्र और मरुत के प्रति उक्तियाँ- काव्य की
दृष्टि से ये सभी वैदिक मानव के विस्मय भाव को ही प्रतिबिम्बित करती
हैं-उस शिशुवत् विस्मय को जिसमें भय का लेश भी नहीं है। ऋग्वेद का
मण्डूक-सूक्त इस विस्मयाह्लाद का उत्तम उदाहरण है।
वाल्मीकि के रामायण में प्रकृति का काव्य-रूप बहुत कुछ बदल गया है।
वाल्मीकि के राम यद्यपि तुलसीदास के मर्यादा-पुरुषोत्तम से भिन्न
कोटि के नायक हैं, तथापि मर्यादा का भाव वाल्मीकि में अत्यन्त पुष्ट
है। बल्कि यह भी कहना अनुचित न होगा कि जिस घटना से आदि-काव्य का
उद्भव माना जाता है वह घटना ही एक मर्यादा अंकित करती है। वास्तव में
क्रौंच-वध वाली घटना में जो लोग शुद्ध कारुण्य देखते हैं वे थोड़ी-सी
भूल करते हैं। आदि-कवि ने क्षुब्ध होकर निषाद को जो शाप दिया था,
उसके मूल में शुद्ध जीव-दया की अपेक्षा मर्यादा-भंग के विरोध का ही
भाव अधिक था। पक्षी मात्र को मारने का विरोध वाल्मीकि ने नहीं किया।
परिस्थिति-विशेष में पक्षी के वध को अधर्म मानकर ही उन्होंने व्याध
की शाश्वत अप्रतिष्ठा की कामना की। उस परिस्थिति में कोई भी प्राणी
अवध्य है, यही विश्वास महाभारत में भी पाया जाता है जो मृगया के
वृत्तान्तों से भरा हुआ है। पांडु की मृत्यु जिस दारुण परिस्थिति में
हुई उसका कारण भी मृगया नहीं थी-मृगया तो राज-धर्म का अंग था-किन्तु
परिस्थिति-विशेष में मृग पर बाण छोडऩे का अधर्म अथवा मर्यादा-भंग ही
राजा के प्राणान्त का कारण हुआ। यह भी उल्लेख्य है कि क्रौंच की कथा
में क्रौंच-युगल को शापग्रस्त मुनि-युगल सिद्ध करना आवश्यक नहीं समझा
गया : वाल्मीकि की करुणा पक्षी को पक्षी मान कर ही दी गयी। किन्तु
महाभारत में राजा के प्राण मृग के प्राण से कदाचित् अधिक मूल्यवान
समझे गए, इसलिए अपराध और दंड में सामंजस्य लाने के लिए मृग-युगल को
मुनि-युगल सिद्ध करना पड़ा। जो हो, यहाँ भी जीव-दया का आत्यन्तिक
आदर्श नहीं है, बल्कि जीव-वध की मर्यादा का ही निर्देश है।
किन्तु जीव-दया के आदर्श के विकास का अध्ययन हमारा विषय नहीं है। हम
प्रकृति के प्रति वाल्मीकि के राग-भाव की, और वैदिक कवि के भाव से
उसके अन्तर की चर्चा कर रहे थे। काव्य-युग में यह अन्तर और भी स्पष्ट
हो जाता है-दूसरे शब्दों में मानवीय दृष्टि के विकास की एक और सीढ़ी
परिलक्षित होने लगती है। शास्त्रीय शब्दावली में यदि कहा जाए कि
प्रकृति काव्य का आलम्बन न रहकर क्रमश: उद्दीपन होती जाती है, तो यह
कथन असंगत तो न होगा, किन्तु बात इतनी ही नहीं है। एक तो
प्रकृति-वर्णन का उद्दीपन के लिए उपयोग वाल्मीकि ने भी
किया-किष्किन्धा-कांड का शरद-वर्णन यद्यपि प्रकृति की दृष्टि से
सच्चा और खरा है तथापि उसके वहाँ होने का मुख्य काव्यगत कारण राम के
पत्नी-विरह को उद्दीपित रूप में हमारे सम्मुख लाना ही है। यही कारण
है कि वह वर्णन जो बिम्ब हमारे सम्मुख उपस्थित करता है वे सभी
शृंगार-भाव से अनुप्राणित हैं। दूसरे, काव्य युग के महारथियों ने
प्रकृति को केवल उद्दीपन रूप में देखा हो, ऐसा भी नहीं है। बल्कि
कालिदास का प्रकृति-पर्यवेक्षण और अध्ययन तथा उनका प्रकृति-प्रेम
भारतीय काव्य-परम्परा में अद्वितीय है।
वास्तव में अन्तर को ठीक-ठीक समझने के लिए जो प्रश्न पूछना होगा वह
यह नहीं है कि प्रकृति के उपयोग में क्या अन्तर आ गया। प्रश्न यह
पूछा चाहिए कि जिस प्रकृति की ओर कवि आकृष्ट था वह प्रकृति कैसी थी?
कालिदास का प्रकृति-प्रेम वाल्मीकि से कम हार्दिक नहीं है। न उनका
काव्य आलम्बन के रूप में प्रकृति को आदि-कवि की रचनाओं से कम महत्त्व
देता है। फिर भी उसमें वाल्मीकि की सी सहजता नहीं है। न वैदिक कवि का
विस्मय भाव ही है। कालिदास की प्रकृति अपेक्षया अलंकृत है। कवि जितना
प्रकृति से परिचित है उतना ही प्रकृति-सम्बन्धी अनेक कवि-समयों से
भी-अर्थात् वह अपने काव्य की परम्परा से भी परिचित है और उस परिचय की
अवज्ञा नहीं करता है। कवि-समय को सत्य वह नहीं मानता, क्योंकि उसका
अनुभव उन्हें मिथ्या सिद्ध करता है; किन्तु फिर भी उन समयों का वह
व्यवहार करता है क्योंकि काव्य-सौन्दर्य के लिए परम्परा से काम लेने
का यह भी एक साधन है। ऋतुसंहार के ऋतु-वर्णन अथवा कुमारसम्भव के
हिमालय-वर्णन में परम्परागत कवि-समयों का कवि के निजी अनुभव के साथ
ऐसा अभिन्न योग हुआ है कि इन तत्त्वों का विश्लेषण सौन्दर्य को नष्ट
किये बिना हो ही नहीं सकता।
आवश्यक परिवर्तन के साथ यही बात भवभूति के प्रकृति-वर्णन के विषय में
भी कही जा सकती है।
वास्तव में काव्य-युग का कवि जो प्रकृति को केवल आलम्बन के रूप में
अपने सम्मुख नहीं रख सका, और न ही उसे निरे उद्दीपन के रूप में एक
उपकरण का स्थान दे सका, उसका कारण यही था कि प्रकृति से उसका सम्बन्ध
भिन्न प्रकार का हो गया था। व्यवस्थित और निरापद जीवन में उसके लिए
यह आवश्यक नहीं रहा था कि प्रकृति की शक्तियों को वैसे आत्यन्तिक और
मानवीकृत अथवा देवतावत् रूपों में देखे जैसे रूप वैदिक कवि के
उद्दिष्ट रहे। दूसरी ओर प्रकृति से उसका सम्बन्ध वैसा उच्छिन्न भी
नहीं हो गया था जैसा रीतिकालीन कवियों का, जिनके निकट प्रकृति केवल
एक अभिप्राय रह गयी थी, और प्रकृति का चित्रण केवल प्रकृति-सम्बन्धी
कवि-समयों की एक न्यूनाधिक चमत्कारी सूची। काव्य-युग के संस्कृत कवि
के लिए प्रकृति शोभन, रम्य और स्फूर्तिप्रद थी। प्राकृतिक शक्ति के
रूप में उसे मानव का प्रतिपक्ष माना जा सकता था, किन्तु अपने इस नये
रूप में वह मानव की सहचरी हो गयी थी।
नि:सन्देह संस्कृत काव्य-परम्परा की समवर्तिनी एक दूसरी
काव्य-परम्परा भी रही जिसकी खोज में हमें प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य
की ओर देखना होगा। संस्कृत और प्राकृत काव्य बराबर एक-दूसरे को
प्रभावित करते रहे; और कवि समयों अथवा अभिप्रायों का आदान-प्रदान
उनमें होता रहा। किन्तु विस्तार से बचने के लिए उनकी चर्चा यहाँ छोड़
दी जा सकती है। ऐसा इसलिए भी अनुचित न होगा कि इसी प्रकार का सम्बन्ध
हम अनन्तर खड़ी बोली हिन्दी की कविता में तथा उसकी पृष्ठभूमि और उसके
परिपाश्र्व में फैले हुए लोक-काव्य में भी देख सकते हैं। इनमें भी
आदान-प्रदान निरन्तर होता रहा, किन्तु इस क्रिया की बढ़ी हुई गति
आधुनिक युग की एक विशेषता मानी जा सकती है। क्यों यह आदान-प्रदान इस
काल में अतिरिक्त तीव्रता के साथ होने लगा, इस प्रश्न का उत्तर भी
हमें आधुनिक संवेदना के रूप-परिवर्तन में मिलेगा। मानव और प्रकृति
दोनों की नयी अवधारणा ने स्वभावतया उनके परस्पर सम्बन्ध को बदल दिया
और इसलिए प्रकृति के वर्णन अथव चित्रण को अनुप्राणित करने वाले
राग-तत्त्व भी बदल गये।
किन्तु बीच की सीढ़ी की उपेक्षा कर जाना भ्रान्ति का कारण हो सकता
है।
प्रकृति-काव्य के विवेचन में वास्तव में समूचे रीति-युग को छोड़ ही
देना चाहिए, क्योंकि रीतिकालीन कवियों में से कुछ ने यद्यपि प्रकृति
के सूक्ष्म पर्यवेक्षण का प्रमाण दिया है, तथापि उनके निकट प्रकृति
काव्य-चमत्कार के लिए उपयोज्य एक साधन-मात्र है। प्रकृति के मानवीकरण
की बात तो दूर, रीति-काल के कवि उसकी स्वतन्त्र इयत्ता के प्रति भी
उदासीन हैं-उनके निकट वह केवल एक अभिप्राय है-अलंकृति के काम आ सकता
है। यह प्रकृति से राग-सम्बन्ध की जर्जरता का ही परिणाम था कि
रीति-कालीन कवि प्राकृतिक तत्त्वों की सूची प्रस्तुत कर देना ही
उद्दीपन के लिए पर्याप्त समझने लगा। यदि उसका राग-सम्बन्ध कुछ भी
प्राणवान होता, तो वह समझता कि प्रकृति-सम्बन्धी शब्दावली का ऐसा
कोशवत उपयोग उद्दीपन का भी काम नहीं कर सकता क्योंकि जिस काव्य में
राग का अभाव स्पष्ट लक्षित होता है वह दूसरे में राग-भाव नहीं जगा
सकता, अपने अभाव को चाहे कितने ही कौशल से छिपाया गया हो। प्रकृति के
बाहरी आकारों की सूची बनाने की यह प्रवृत्ति रीति-काल तक ही सीमित
नहीं रही बल्कि आधुनिक काल तक चली गयी। बीसवीं शती में भी जो
महाकाव्य लिखे गये वे अधिकतर प्रकृति-वर्णन की इसी लीक को पकड़े रहे
और पिंगल-ग्रन्थों ने भी अभ्यासियों के लिए विभावों की सूचियाँ
प्रस्तुत कीं।
वास्तव में इस जीर्ण परम्परा से विमुख होकर प्रकृति को काव्य में नये
प्राण देने की प्रवृत्ति हिन्दी में पश्चिमी साहित्य के अथवा उससे
प्रभावित बांग्ला साहित्य के सम्पर्क से जागी। इस कथन का अभिप्राय यह
कदापि नहीं है कि खड़ी बोली का प्रकृति-वर्णन अनुकृति है, क्योंकि
अनुकृति का विरोध ही तो इसकी प्रेरणा रही। अभिप्राय यह भी नहीं है कि
हिन्दी कवि अपने पूर्वजों की अनुकृति छोडक़र विदेशी कवियों की अनुकृति
करने लगे, क्योंकि हिन्दी की नयी प्रवृत्ति प्राचीनतर भारतीय
परम्पराओं से कटी हुई कदापि नहीं थी। बल्कि उदाहरण देकर दिखाया जा
सकता है कि कैसे छायावाद के और परवर्ती प्रमुख कवियों ने पूरे
आत्म-चेतन भाव से संस्कृत काव्यों से और वैदिक साहित्य से न केवल
प्रेरणा पायी वरन उपमाएँ और बिम्ब ज्यों के त्यों ग्रहण किये।
पश्चिमी साहित्य से प्रेरणा पाने का आशय यह भी नहीं है कि यदि पश्चिम
से सम्पर्क न हुआ होता तो हिन्दी साहित्य में प्रकृति की नयी चेतना न
जागी होती। वास्तव में किसी भी प्रवृत्ति के बारे में यह नहीं कहा जा
सकता कि वह किसी विशेष साहित्य में कभी नहीं प्रकट होगी। जो साहित्य
जीवित है-अर्थात् जिस साहित्य को रचनेवाला समाज जीवित है-उसमें
समय-समय पर जीर्णता का विरोध करनेवाली नयी प्रवृत्तियाँ प्रकट होंगी
ही। दूसरे साहित्यों से प्रभाव ग्रहण करने की भी एक क्षमता और
तत्परता होनी चाहिए जो हर साहित्य में हर समय वर्तमान नहीं होती
बल्कि विकास अथवा परिपक्वता की विशेष अवस्था में ही आती है। इसलिए
किसी प्रभाव से जो रचनात्मक प्रेरणा मिली, उसे अनुकृति कहना या हेय
मानना अनुचित है और बहुधा ऐसी समालोचना करने वाले के आत्मावसाद अथवा
हीनभाव का ही द्योतक होता है। शिशु बोलना अनुकरण से सीखता है, किन्तु
कवि-समुदाय में रख देने से ही बालक कविता नहीं करने लगता। जब वह
कविता रचता है तो वह इतने भर से अनुकृति नहीं हो जाती कि वह कवियों
के सम्पर्क में रहा और उनसे प्रभाव ग्रहण करता रहा। उसकी ग्रहणशीलता
और उस पर आधारित रचना-प्रवृत्ति स्वयं उसके विकास और उसकी शक्ति के
द्योतक हैं।
पश्चिमी काव्य के परिचय से भारतीय कवि एक बार फिर प्रकृति की
स्वतन्त्र सत्ता की ओर आकृष्ट हुआ। कहा जा सकता है कि इसी परिचय के
आधार पर वह स्वयं अपनी परम्परा को नयी दृष्टि से देखने लगा और उसके
सार तत्त्वों को नया सम्मान देने लगा। नि:सन्देह अनुकरण भी हुआ,
किन्तु जो केवल मात्र अनुकरण था वह कालान्तर में उसी गौण पद पर आ गया
जो उसके योग्य था। उषा-सुन्दरी का मानवी रूप छायावादियों का आविष्कार
नहीं था, और उसकी परम्परा ऋग्वेद तक तो मिलती ही है। किनतु जब कवि ने
छाया को भी मानवी आकृति देकर पूछा :
कौन, कौन तुम,
परिहत-वसना
म्लानमना, भू-पतिता-सी?
तब उसके अवचेतन में वैदिक
परम्परा उतनी नहीं रही होगी जितना अँग्रेज़ी रोमांटिक काव्य जिसमें
प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण साधारण बात थी।
किन्तु नयापन केवल इतना नहीं था-पुरानेपन का नया सँवार-भर नहीं था।
मानवीकरण केवल विषयाश्रित नहीं था। बल्कि प्रकृति के मानवीकरण का
विषयिगत रूप और भी अधिक महत्त्वपूर्ण था।
मानवीकरण का यह पक्ष वास्तव में वैयक्तिकीकरण का पक्ष था। यही तत्त्व
था जिसने प्रकृति-वर्णन को प्राकृतिक अभिप्रायों के वर्णन से अलग
करके काव्योचित दृष्टि को रूप दे दिया। यद्यपि नये जागरण ने हिन्दी
कविता का सम्बन्ध रीतिकाल के अन्तराल के पार अपभ्रंशों, प्राकृतों और
संस्कृत काव्य की परम्परा से जोड़ा था, तथापि इसके आधार पर जो
दृश्य-चित्र सामने आये थे नये होकर भी इस अर्थ में एक-रूप थे कि
विभिन्न कवियों के द्वारा प्रस्तुत किए गये होने पर भी वे मूलत: समान
थे-ऐसा नहीं था कि उस विशेष कवि के व्यक्तित्व से उन्हें अलग किया ही
न जा सके। दार्शनिक पृष्ठिका के विचार से कहा जा सकता है कि
सुमित्रानन्दन पन्त ने प्रकृति की कल्पना प्रेयसी के रूप में की और
‘निराला’ ने संवाहिका शक्ति के रूप में और दोनों कवियों के
प्रकृति-चित्रण में समानता और अन्तर दोनों ही पहचाने जा सकते हैं।
किन्तु जिस व्यक्तिगत अन्तर की बात हम कह रहे हैं वह इससे गहरा था।
नि:सन्देह काव्यगत चित्रों पर कवि के व्यक्तित्व के इस आरोप का
अध्ययन पश्चिमी साहित्यके सन्दर्भ में किया जा सकता है और दिखाया जा
सकता है कि उसमें भी अँग्रेज़ी रोमांटिक काव्यके व्यक्तिवाद का कितना
प्रभाव था। और यदि व्यक्तिवाद के विकृत प्रभावों को ही ध्यान में रखा
जाए तो यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि पश्चिमी प्रभाव यहाँ भी
विकृतियों का आधार बना, जैसा कि वह पश्चिम में भी बना था। किन्तु
किसी प्रभाव का केवल उसकी विकृतियों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया
जा सकता। और रोमांटिक व्यक्तिवाद का स्वस्थ प्रभाव यह था कि उसने
प्रकृति के चित्रों को एक नयी रागात्मक प्रामाणिकता दी। जो तथ्य था
और सबका ‘जाना हुआ’ था उसे उसने एक व्यक्ति का ‘पहचाना हुआ’ बनाकर
उसे सत्य में परिणत कर दिया। जहाँ यह व्यक्तिगत दर्शन केवल
असाधारणत्व की खोज हुआ-और यह प्रवृत्ति पश्चिम में भी लक्षित हुई
जैसी कि हिन्दी के कुछ नये कवियों में-वहाँ उत्तम काव्य का निर्माण
नहीं हुआ। जैसा कि रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है :
‘केवल असाधारणत्व-दर्शन की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है।’
किन्तु जहाँ व्यक्तिगत दर्शन ने उस पर खरी अनुभूति की छाप लगा दी
वहाँ उसके देखे हुए बिम्ब और दृश्य अधिक प्राणवान और जीवनस्पन्दित हो
उठे। यह भी रामचन्द्र शुक्ल का ही कथन है कि :
‘वस्तुओं के रूप और आस-पास की वस्तुओं का ब्यौरा जितना ही स्पष्ट या
स्फुट होगा उतना ही पूर्ण बिम्ब ग्रहण होगा और उतना ही अच्छा
दृश्य-चित्रण कहा जाएगा।’
और यह व्यक्तिगत दर्शन या निजी अनुभूति की तीव्रता ही है जो वस्तुओं
के रूप को ‘स्पष्ट या स्फुट’ करती है। प्रकृति के जो चित्र रीति-काल
के कवि प्रस्तुत करते थे, वे भी यथातथ्य होते थे। उस काव्य की
समवर्तिनी चित्र-कला में शिकार इत्यादि के जो दृश्य आँके जाते थे वे
भी उतने ही रीतिसम्मत और यथातथ्य होते थे। किन्तु व्यक्तिगत अनुभूति
का स्पन्दन उनमें नहीं होता था और इसीलिए उनका प्रभाव वैसा
मर्मस्पर्शी नहीं होता था। बाँसों के झुरमुट पहले भी देखे गए थे,
किन्तु सुमित्रानन्दन पन्त ने जब लिखा-
बाँसों का झुरमुट
सन्ध्या का झुटपुट
हैं चहक रही चिडिय़ाँ :
टी-वी-टी-टुट्-टुट्।
तब यह एक झुरमुट बाँसों के
और सब झुरमुटों से विशिष्ट हो गया, क्योंकि व्यक्तिगत दर्शन और
अनुभूति के खरेपन ने उसे एक घनीभूत अद्वितीयता दे दी। इस प्रकार के
उदाहरण ‘निराला’और पन्त की कविताओं से अनेक दिये जा सकते हैं।
परवर्ती काव्य में भी वे प्रचुरता से मिलेंगे, भले ही उनके साथ-साथ
निरे असाधारणत्व के मोह के भी अनेक उदाहरण मिल जाएँ। जब हम
दृश्य-चित्रण की परम्परा का अध्ययन इस दृष्टि से करते हैं तो यह
स्पष्ट हो जाता है कि छायावाद ने प्रकृति को एक नया सन्दर्भ और अर्थ
दिया, जो उसे न केवल उससे तत्काल पहले के खड़ी बोली के युग से अलग
करता है बल्कि खड़ी बोली के उत्थान से पहले के सभी युगों से भी अलग
करता है। सुमित्रानन्दन पन्त और सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ इस नये
पथ के शलाका-पुरुष हैं, किन्तु इसके पूर्व संकेत श्रीधर पाठक और
रामचन्द्र शुक्ल के प्रकृति काव्य में ही मिलने लगते हैं।
नयी कविता, जहाँ तक प्रकृति-चित्रों के अनुभूतिगत खरेपन की बात है,
छायावाद से अलग दिशा में नहीं गयी है। असाधारण की खोज के उदाहरण
उसमें अधिक मिलेंगे और तन्त्र का कच्चापन अथवा भाषा का अटपटापन भी
कहीं अधिक। बल्कि भाषा के विषय में एक प्रकार की अराजकता भी लक्षित
हो सकती है, जिसका विस्तार ‘लोक-साहित्य की ओर उन्मुखता’ या ‘लोक के
निकटतर पहुँचने के लिए बोलियों से शब्द ग्रहण करने की प्रवृत्ति’ की
ओट लेने पर भी छिप नहीं सकता। पल्लव की भूमिका में पन्त ने जिस
सूक्ष्म शब्द-चेतना का परिचय दिया था, भाषा के व्यवहार के प्रति वैसा
जागरूक भाव नयी कविता के बिरले कवियों में ही मिलेगा (छायावाद-युग
में भी ऐसे कवि कम विरल नहीं थे; अराजकता ऐसी नहीं थी)। ये दोष उन
नयी प्रवृत्तियों का ऋण पक्ष हैं जो कि नये काव्य को अनेक समानताओं
के बावजूद छायावाद के काव्य से पृथक् करती हैं।
किन्तु जहाँ तक प्रकृति-वर्णन और प्रकृति-चित्रण का प्रश्न है, नयी
कविता की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ सब ऋण-मूलक ही नहीं हैं, न उसका धन
पक्ष छायावाद से सर्वथा एकरूप। उसकी विशिष्टता को ठीक-ठीक पहचानने के
लिए हमें फिर अपने तत्सम्बन्धी प्रश्न के सही निरूपण पर बल देना
होगा। प्रकृति के उपयोग में क्या अन्तर आया, यह प्रश्न भी अप्रासंगिक
नहीं है; पर मूल्यों को ठीक-ठीक समझने के लिए इससे गहरे जाकर फिर यही
प्रश्न पूछना चाहिए कि जिस प्रकृति की ओर कवि आकृष्ट है वह प्रकृति
कैसी है?
स्पष्ट है कि आज का कवि जिस प्रकृति से परिचित होगा वह उससे भिन्न
होगी जो आरण्यक कवियों की परिचित रही। यह नहीं कि वन-प्रदेश आज नहीं
है, या झरने नहीं बहते, या मृग-छौने चौकड़ी नहीं भरते, या
ताल-सरोवरों में पक्षी किलोलें नहीं करते। पर आज के कस्बों और शहरों
में रहने वाले कवि के लिए ये सब चित्र अपवाद-रूप ही हैं। केवल इन्हीं
का चित्रण करने वाला लेखक एक प्रकार का पलायनवादी ही ठहरेगा-क्योंकि
वह अपने अनुभूत के मुख्यांश की उपेक्षा में एक अप्रधान अंश को तूल दे
रहा होगा। इतना ही नहीं, अनेकों के लिए तो गाँव-देहात के दृश्य भी
इनकी अपेक्षा कुछ ही कम अपरिचित होंगे, और उन्हें ‘अहा ग्राम्य जीवन
भी क्या है!’ जैसे वर्णन न केवल काव्य की दृष्टि से घटिया लगेंगे
बल्कि उनकी अनुभूति भी चेष्टित और अयथार्थ लगेगी। भारत का
कृषि-प्रधानत्व अब भी मिटा नहीं है और इसलिए यह प्राय: असम्भव है कि
किसी भारतीय कवि ने खेत देखे ही न हों, पर ‘खेत देखे हुए’ होने और
‘देहाती प्रकृति का अनुभव रखने’ में अन्तर वैसा नगण्य नहीं है।
अनुभव-सत्यता पर-व्यक्तिगत अनुभूति के खरेपन पर जो आग्रह छायावाद ने
आरम्भ किया था-काव्य के परम्परागत अभिप्रायों और ऐतिहासिक पौराणिक
वृत्त को ही अपना विषय न मान कर, अनुभूति-प्रत्यक्ष और
अन्तश्चेतन-संकेतित को सामने लाना छायावादी विद्रोह का एक रूप रहा-यह
नयी कविता में भी वर्तमान है। पर कृतिकारत्व जब समाज के किसी विशिष्ट
सुविधा-सम्पन्न अंग तक सीमित नहीं रहा है, तब यह सच्चाई का आग्रह ही
कवि के क्षेत्र को मर्यादित भी करता है। जिस गिरि-वन-निर्झर के
सौन्दर्य को संस्कृत का कवि किसी भी प्रदेश में मूर्त कर सकता था,
उसे यथार्थ में प्रतिष्ठित करने के लिए आज कवि पहले आपको मसूरी की
सैर पर ले जाता है या नैनीताल की झील पर, या कश्मीर या दार्जिलिंग;
जिस ग्राम-सुषमा का वर्णन खड़ी बोली के कवि इस शती के आरम्भ में भी
इतने सहज भाव से करते थे, उसे सामने लाने से पहले कवि अपने प्रदेश
अथवा अंचल की सीमा-रेखा निर्धारित करने को बाध्य होता है-क्योंकि वह
जानता है कि प्रत्येक अंचल का ग्राम-जीवन विशिष्ट है और एक का अनुभव
दूसरे को परखने की कसौटी नहीं देता-और यही कारण है कि नयी कविता के
प्रकृति-वर्णन में ऐसे दृश्यों का वर्णन अधिक होने लगा है जो किसी हद
तक प्रादेशिकता से पूरे हो सकते हैं-जो प्रकृति-क्षेत्र की
‘आत्यन्तिक’ घटनाएँ हैं-सूर्योदय, सूर्यास्त, बरसात की घटा,
आँधी...इतना ही नहीं, उसमें गोचर अनुभवों का विपर्यय भी अधिक होता
है। यथा, ‘दृश्य’ को ‘मूर्त’ करने के लिए वह जो अनुभूति ‘चित्र’
हमारे सम्मुख लाता है। उसका आधार दृष्टि (अथवा घ्राण) न हाकर स्पर्श
हो जाता है-अर्थात् वह ‘दृश्य’ रहता ही नहीं। वसन्त के वर्णन में
फूलों-कोपलों का ‘स्पष्ट और स्फुट ब्यौरा’ देने चलते ही एक प्रदेश
अथवा क्षेत्र के साथ बँध जाना पड़ता, और यही बात गन्धों की चर्चा से
होती; पर वसन्त को यदि केवल धूप की स्निग्ध गरमाई के आधार पर ही
अनुभूति-प्रत्यक्ष किया जा सके तो प्रादेशिक सीमा-रेखाएँ क्यों खींची
जाएँ?
नि:सन्देह अति कर जाने पर यही प्रवृत्ति स्वयं अपनी शत्रु हो जा सकती
है और अनुभूति-सत्यता तथा व्यापकता का द्विमुख आग्रह फिर ऐसी स्थिति
ला सकता है जिसमें कविता यन्त्रवत् कुशलता के साथ बने-बनाये
अभिप्रायों का निरूपण, रक्त-माँस-हीन बिम्बों और प्रतीकों का सृजन हो
जाए। प्रतीक ही नहीं, बिम्ब भी कितनी जल्दी प्रभावहीन, निष्प्राण
अभिप्राय-भर हो जाते हैं, समकालीन साहित्य में नागफनी, कैक्टस और
गुलमोहर की छीछालेदर इसका शिक्षाप्रद उदाहरण है? पर अभी तो खतरा
अधिकतर सैद्धान्तिक है, और अभी नयी कविता के सम्मुख अपने को अपनी
प्रकृति के अनुरूप बनाने के प्रयत्न के लिए काफ़ी खुला क्षेत्र है।
बल्कि अभी तो व्यापक प्रतीकों की इस खोज की और अल्पसंख्य कवि ही
प्रवृत्त हुए हैं, और प्रामाणिकता का आग्रह आँचलिक, प्रादेशिक अथवा
पारिवेशिक प्रवृत्तियों में ही प्रतिफलित हो रहा है।
नयी काव्य प्रवृत्तियों को सामने रख कर एक अर्थ में कहा जा सकता है
कि प्रकृति-काव्य अब वास्तव में है ही नहीं। एक विशिष्ट अर्थ में यह
भी कहा जा सकता है कि छायावाद का प्रकृति-काव्य अपनी सीमाओं के
बावजूद अन्तिम प्रकृति-काव्य था; यदि छायावादी काव्य मर गया है तो
उसके साथ ही प्रकृति-काव्य की अन्त्येष्टि भी हो चुकी है। किन्तु ऊपर
के निरूपण से यह स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसा एक विशिष्ट अर्थ में ही
कहा जा सकता है; और यह विशेषता नये प्रकृति-काव्य का शील-निरूपण करने
में सहायक होती है।
छायावाद के लिए ‘प्रकृति’ मानवेतर यथार्थ का पर्याय नहीं थी, मानव के
साथ मानव-निर्मिति को छोडक़र शेष जगत भी उसकी प्रकृति नहीं था। बल्कि
इस शेष में जो सुन्दर था, जो सौष्ठव-सम्पन्न था, जो ‘रूप’-सम्पन्न
था, वही उसका लक्ष्य था। शास्त्रीय (क्लासिकल) दृष्टि में प्रकृति की
हर क्रिया और गति-विधि एक व्यापक नियम अथवा ऋतु की साक्षी है;
छायावाद की दृष्टि ऋतु की अमान्य नहीं करती थी, पर उसका आग्रह
रूप-सौष्ठव पर था। नयी कविता के रूप का आग्रह कम नहीं है, पर उसने
सौष्ठव वाले पक्ष को छोड़ दिया है, तद्वत्ता पर ही वह बल देती है।
‘व्यवस्थित संसार’ के स्थान में ‘सुन्दर संसार’ की प्रतिष्ठा हुई थी;
अब उसके स्थान में ‘तद्वत संसार’ ही सामने रखा जाता है। इतना ही
नहीं, मानव-निर्मिति को भी उससे अलग नहीं किया जाता-क्योंकि ऐसी
असम्पृक्त प्रकृति अब दीखती ही कहाँ है!
इस प्रकार प्रकृति-वर्णन का वृत्त कालिदास के समय से पूरा घूम गया
है। कालिदास ‘प्रकृति के चौखटे में मानवी भावनाओं का चित्रण’ करते
थे; आज का कवि ‘समकालीन मानवीय संवेदना के चौखटे में प्रकृति’ को
बैठाता है। और, क्योंकि समकालीन मानवीय संवदेना बहुत दूर तक विज्ञान
की आधुनिक प्रवृत्ति से मर्यादित हुई है, इसलिए यह भी कहा जा सकता है
कि आज का कवि प्रकृति को विज्ञान की अधुनातन अवस्था के चौखटे में भी
बैठाता है। ऋतु का स्थान वैज्ञानिक शोध ने ले लिया है। किन्तु ऋतु
सनातन और आत्यन्तिक था, वैज्ञानिक शोध के दिङ्मान बदलते हैं... फलत:
‘प्रकृति का सान्निध्य’ नये कवि को पहले का-सा आश्वस्त भाव नहीं
देता, उसकी आस्थाओं को पुष्ट नहीं करता-इसके लिए वह नये प्रतीकों की
खोज करता है। पर प्रतीकों की रचना के-उनकी अर्थवत्ता के विकास और
ह्रास के-अन्वेषण का क्षेत्र, चेतन और अवचेतन के सम्बन्धों का
क्षेत्र है; जो जोखम-भरा भी है और केवल प्रकृति-काव्य के
रूप-परिवर्तन के वर्णन के लिए अनिवार्य भी नहीं है, अत: उसमें भटकना
असामयिक होगा।
किन्तु प्रस्तुत संकलन-ग्रन्थ के प्रणयन की मूल प्रेरणा को ध्यान में
रखते हुए कदाचित् इतना कहना उचित होगा कि यदि इस विशेष अर्थ में
छायावाद वस्तुत: अन्तिम प्रकृति-काव्य था, तो सुमित्रानन्दन पन्त
स्वभावत: युग-कवि रहे। अथवा-ऐसा श्लेष इस प्रसंग में क्षन्तव्य हो
तो-यह कहा जाए कि पन्त और ‘निराला प्रकृति-काव्य के अन्तिम युग के
युग-कवि रहे। हमारे सौभाग्य से दोनों ही कवि हमारे मध्य में रहे हैं,
यद्यपि छायावाद का युग बीत चुका माना जाता है। किन्तु युग-कवि का युग
को अतिक्रान्त करना ही स्वाभाविक है।
सुमित्रानन्दन पन्त की अद्यतन रचनाएँ उन प्रकृतियों के प्रतिकूल नहीं
हैं जिनकी हम उनकी रचनाओं से परवर्ती काल के लिए उद्भावना करते, यह
उनकी दृष्टि के खरेपन का ही प्रमाण है।
|
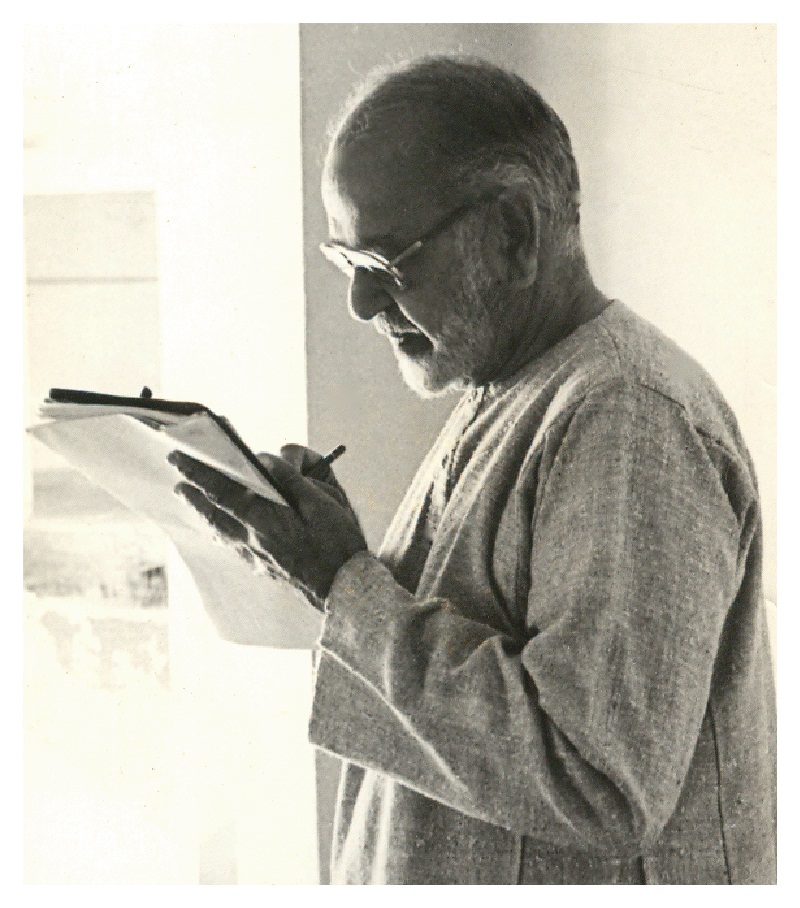
No comments:
Post a Comment